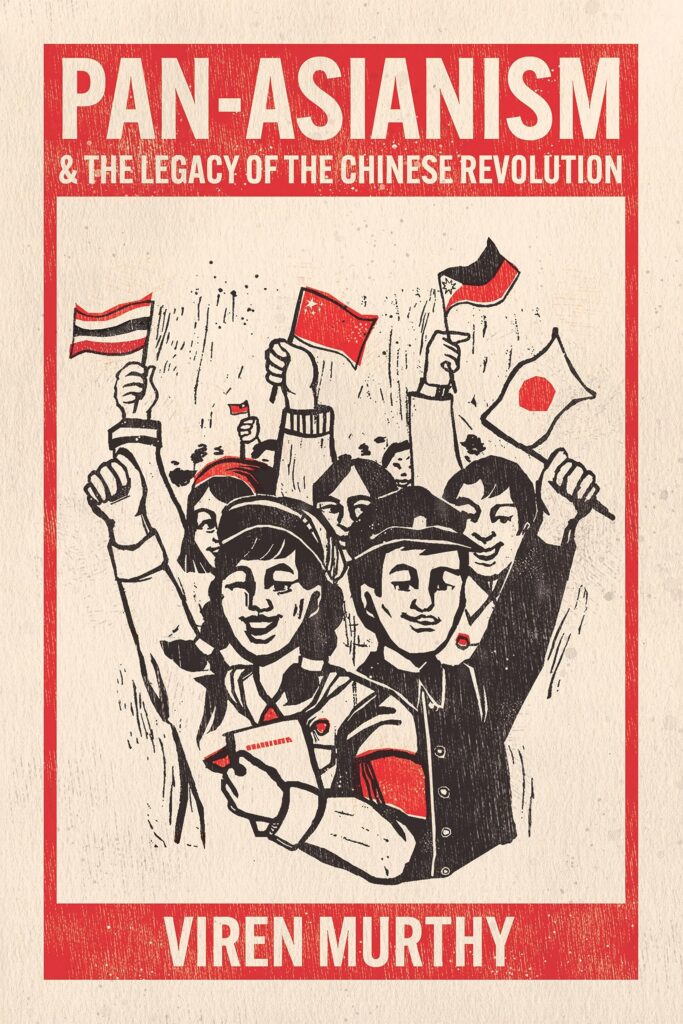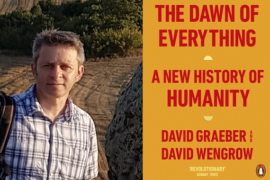इस महीने हुए यूरोपीय संसद के चुनावों का सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि लोगों ने जिस नतीजे की उम्मीद लगाई हुई थी अंत में वाकई वही नतीजा निकला। मार्क्स ब्रदर्स के एक क्लासिक दृश्य से उधार लेकर कहूं, तो: यूरोप जैसी बातें और जैसा बरताव कर रहा था उससे ऐसा लगता रहा होगा कि वह धुर दक्षिणपंथ की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको इस चक्कर में मूर्ख नहीं बनना चाहिए; यूरोप वास्तव में धुर दक्षिणपंथ की ओर ही जा रहा है।
इस बात पर जोर देने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुख्यधारा का ज्यादातर मीडिया इसे दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमें वहां यही सुनाई पड़ता रहता है कि ‘’बेशक मरीन ली पेन, जॉर्जिया मेलोनी और आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) कभी-कभार फासिस्ट मंशाओं के साथ गलबहियां करते दिखते हैं पर इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि सत्ता में आने के बाद वे अब भी लोकतांत्रिक नियमों और संस्थाओं का सम्मान करते हैं।‘’ धुर दक्षिणपंथ को इस तरीके से पालने में खिलाया जाना हम सब के लिए परेशानी वाली बात होनी चाहिए क्योंकि यह परंपरागत कंजर्वेटिव दलों के नई लहर पर सवार होने की तैयारी का संकेत है। ‘’फासिस्टों के साथ कोई गठबंधन नहीं’’- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय लोकतंत्र द्वारा अपनाई गई इस सूक्ति को चुपचाप तिलांजलि दी जा चुकी है।

इस चुनाव का संदेश एकदम साफ है। अब यूरोपीय संघ के ज्यादातर देशों के बीच राजनीतिक विभाजन नरम दक्षिणपंथ और नरम वामपंथ का नहीं रह गया है। अब यह परंपरागत दक्षिणपंथ (जिसकी नुमाइंदगी चुनाव जीतने वाली यूरोपियन पीपुल्स पार्टी ईपीपी करती है जिसमें ईसाई डेमोक्रेट, लिबरल-कंजर्वेटिव और परंपरागत कंजर्वेटिव हैं) और नए फासिस्टों (जिसके प्रतिनिधि ली पेन, मेलोनी और एएफडी इत्यादि हैं) के बीच का मामला बन चुका है।
अब सवाल बस इतना है कि ईपीपी क्या नए फासिस्टों के साथ गठजोड़ करेगी। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियेन इस चुनाव के परिणाम को दोनों ‘’अतियों’’ के खिलाफ ईपीपी की विजय के रूप में प्रचारित करने में जुटी हुई हैं, बावजूद इसके नई संसद के भीतर अब एक भी वाम धारा की पार्टी नहीं बैठेगी जबकि इनका अतिवाद धुर दक्षिणपंथ के अतिवाद के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। ईयू की शीर्ष अधिकारी की तरफ से ऐसा ‘’संतुलित’’ विचार शैतानी इशारे कर रहा है।
आज फासीवाद पर बात करते हुए हमें खुद को केवल विकसित पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसी किस्म की राजनीति ग्लोबल साउथ (दक्षिणी गोलार्द्ध) के ज्यादातर देशों में भी उभार पर है। चीन के विकास पर किए अपने अध्ययन में इटली के मार्क्सवादी इतिहासकार दोमेनिको लेसुर्दो (जो स्टालिन की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए भी जाने जाते हैं) आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच फर्क बरतने पर बहुत जोर देते हैं। वे बताते हैं कि अपने आर्थिक ‘’सुधारों’’ को लागू करते समय देंग शाओपिंग को अच्छे से पता था कि एक समाज की उत्पादक शक्तियों को मुक्त करने के लिए पूंजीवादी तत्व अनिवार्य होते हैं, लेकिन वे इस पर बात पर जोर देते रहे कि राजनीतिक सत्ता तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही मजबूती से कायम रहनी चाहिए (ताकि वह मजदूरों और किसानों की स्वयंभू प्रतिनिधि बनी रहे)।
इस नजरिये की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। करीब एक सदी से ज्यादा वक्त से चीन ने ‘’अखिल-एशियाई’’ नजरिया अपनाया हुआ है। यह दृष्टि उन्नीसवीं सदी के अंत में पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व और शोषण की प्रतिक्रिया में उभरी थी। इतिहासकार विरेन मूर्ति जैसा कि बताते हैं, यह परियोजना हमेशा से पश्चिम के लिबरल व्यक्तिवाद और साम्राज्यवाद के अस्वीकार से संचालित थी, पश्चिमी पूंजीवाद के अस्वीकार से नहीं। अखिल-एशियाई दृष्टि के पैरोकारों का मानना रहा है कि प्राक्-आधुनिक परंपराओं और संस्थाओं के आधार पर एशिया के समाज खुद अपना आधुनिकीकरण कर पाने में समर्थ हैं जिसके सहारे वे पश्चिम से कहीं ज्यादा गतिमान हो सकते हैं।
खुद हीगेल भी एशिया को ठस व्यवस्था वाला एक समाज मानते थे जो व्यक्तिवाद (मुक्त आत्मपरकता) की छूट नहीं देता। अखिल-एशियावाद के प्रवर्तकों ने एक नई हीगेलियन अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी व्यक्तिवाद में मिलने वाली स्वतंत्रता चूंकि अंतत: व्यवस्था के खिलाफ जाती है और समाज को तोड़ने का काम करती है, तो स्वतंत्रता को बचाए रखने का इकलौता तरीका यह है कि उसे एक नए किस्म की सामूहिकता और सामूहिक कृत्य की दिशा में ठेल दिया जाए।
इस मॉडल का एक आरंभिक उदाहरण हमें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान के सैन्यकरण और औपनिवेशिक विस्तार में देखने को मिलता है, लेकिन इतिहास के सबक हम बहुत जल्द भुला देते हैं। बड़ी-बड़ी समस्याओं के समाधान की तलाश में लगे पश्चिम में हो सकता है कई लोग वैयक्तिक प्रेरणाओं को निगल जाने और सामूहिक परियोजनाओं में अर्थ खोजने वाले एशियाई मॉडल की ओर आकृष्ट हो रहे हों।
अखिल-एशियावाद का विचार हमेशा ही अपने समाजवादी और फासीवादी संस्करणों के बीच झूलता रहा है। दोनों संस्करणों के बीच विभाजक रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं रही। इससे समझ आता है कि ‘’साम्राज्यवाद-विरोध’’ उतना मासूम भी नहीं है जितना दिखता है। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जापानी और जर्मन फासिस्ट खुद को लगातार अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्यवाद के खिलाफ एक रक्षक के रूप में पेश किया करते थे। आज हम पाते हैं कि यूरोपीय संघ के बरअक्स धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता बिलकुल यही पोजीशन ले रहे हैं।
यह भी पढ़ें
अमेरिका से लेकर भारत तक अपने नेता के साये में जॉम्बी बनते राजनीतिक दल
क्या 2024 पूरी दुनिया में ‘कब्जे का वर्ष’ है? क्या 1933 खुद को दोहरा रहा है?
यही रवैया देंग के बाद उभरे चीन में दिखता है, जिसे राजनीतिविज्ञानी ए. जेम्स ग्रेगोर ‘’समकालीन फासीवाद का ही एक संस्करण’’ मानते हैं- एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे एक निरंकुश राज्य नियंत्रित और संचालित करता है, जिसकी वैधता जातीय परंपराओं और राष्ट्रीय विरासत के चौखटे में परिभाषित होती है। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा चीन के लंबे, निरंतर और प्राचीन इतिहास का हवाला देते हैं। राष्ट्रवादी परियोजनाओं के हित में आर्थिक आवेगों का दोहन करना ही तो फासीवाद की बुनियादी परिभाषा है! राजनीति की बिलकुल ऐसी ही गति हम भारत, रूस, तुर्की और दूसरे देशों में भी देखते हैं।
यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस मॉडल की इतनी अपील क्यों है। सोवियत रूस तो बिखर गया, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कठोर नियंत्रण कायम रखते हुए आर्थिक उदारीकरण को अपनाया। जो वामपंथी चीन को हमदर्दी के साथ देखते हैं, वे इसीलिए उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसने पूंजी को अपने मातहत कर रखा है जबकि इसके ठीक उलट, अमेरिका और यूरोप के तंत्र में पूंजी का राज ही सर्वोपरि है।
नए फासीवाद में दो और रुझान सहयोग कर रहे हैं। यूरोप के चुनाव में ली पेन के बाद एक अन्य बड़े विजेता साइप्रस के मशहूर यूट्यूबर फिदियास पनाइयोतू हैं, जिन्होंने एलन मस्क को गले लगाने की कोशिश कर के सुर्खियां बंटोरी थीं। ट्विटर मुख्यालय के बाहर मस्क के आने का इंतजार करते हुए उन्होंने अपने फॉलोवर्स को अपनी यह इच्छा मस्क की मां तक ‘स्पैम’ संदेशों से पहुंचाने को कह दिया था। आखिरकार मस्क आए, पनाइयोतू से मिले और उन्हें गले भी लगाया। इसके बाद पनाइयोतू ने यूरोपीय संसद के चुनावों में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर डाली। बिना किसी पार्टी के उन्होंने चुनाव लड़ा और 19.4 प्रतिशत पॉपुलर वोट लेकर संसद में अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली।

फ्रांस, यूके, स्लोवीनिया और दूसरी जगहों पर भी कुछ ऐसे ही चेहरे उभर कर आए हैं। अपनी उम्मीदवारी के पीछे इन सभी का एक ‘’लेफ्टिस्ट’’ तर्क था कि चूंकि लोकतांत्रिक राजनीति मजाक बन चुकी है, तो अब मसखरे भी चुनाव लड़ ही सकते हैं। यह खेल बहुत खतरनाक है। जितने ज्यादा लोग मुक्ति की राजनीति से हताश होकर मसखरेपन की ओर जाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे, नव-फासीवाद के लिए राजनीतिक जगह उतनी ही ज्यादा बनती जाएगी।
इस जगह पर दावा करना और इसे वापस हासिल करना अब गंभीर और वास्तविक कार्रवाई की मांग करता है। फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां के साथ मेरी तमाम असहमतियों के बावजूद मुझे लगता है कि उन्होंने धुर दक्षिणपंथ की विजय की प्रतिक्रिया में नेशनल असेंबली को भंग कर के और फिर से चुनाव करवाने की मांग उठा के सही काम किया है। उनके यह घोषणा करते ही हर किसी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई।
बेशक यह काफी जोखिम भरा काम है लेकिन यह खतरा उठाने के काबिल भी है। हो सकता है कि जीतने के बाद ली पेन नए प्रधानमंत्री का नाम खुद तय करें, लेकिन राष्ट्रपति के बतौर मैक्रां उस सरकार के खिलाफ बहुमत को एकजुट करने का सामर्थ्य फिर भी अपने पास कायम रखेंगे। हमें इस लड़ाई को नव-फासीवाद के खिलाफ मुकम्मल करना ही होगा- जितनी मजबूती से हो सके और जितना भी तेज।
Copyright: Project Syndicate, 2024.
www.project-syndicate.org