इतिहास पर वर्गीय नजरिये से काम करने वाला एक इतिहासकार खेतिहर वर्ग को अकेले जितना केंद्र में रख सकता है, मेरे खयाल से हमें भी उत्पीड़ित लैंगिकता पर उससे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हमारा लक्ष्य लैंगिकताओं की अहमियत को समझना है, ऐतिहासिक अतीत में लैंगिक समूहों के महत्व को समझना है।
नताली ज़ेमोन डेविस
नताली ज़ेमोन डेविस का 1975 का यह कथन जेंडर (लैंगिकता) के अध्ययन में मर्दों का विश्लेषण एक वर्चस्वशाली समूह के रूप में किए जाने की वकालत करता है। अतीत में किए गए जेंडर से जुड़े अध्ययनों के केंद्र में काफी लम्बे अरसे तक सिर्फ औरतें रही हैं। जेंडर से जुड़े अध्ययन-जगत को डेविस की यह बात समझते-समझते बीसवीं सदी का पूरा उत्तरार्द्ध बीत गया। तब कहीं जाकर बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में जेंडर-अध्ययनों के केंद्र में पुरुषों को जगह मिली।
जेंडर-अध्ययन में सम्पूर्णता लाने के लिहाज से यह बेहद आवश्यक था कि महज ‘उत्पीड़ित’ नहीं, बल्कि ‘उत्पीड़क’ का भी अध्ययन किया जाए ताकि एक सामाजिक संरचना के रूप में जेंडर की गुत्थी को ठीक ढंग से समझा जा सके। अध्येताओं एवं शोधार्थियों द्वारा इस तर्क को आत्मसात करने के चलते ही बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में ‘मैस्कुलिनिटी’ यानी मर्दानगी पर केन्द्रित अध्ययनों की बाढ़-सी आ गई थी। भारत में इस कड़ी में पहला संजीदा काम आशीष नंदी की किताब द इंटिमेट एनेमी मानी जाती है। उसके बाद तो कई भारतीय अध्येताओं एवं शोधार्थियों ने मर्दानगी को केंद्र में रखकर विपुल लेखन किया।
सबाल्टर्न यानी निम्नवर्गीय इतिहास के प्रोजेक्ट के संस्थापकों में एक प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पाण्डेय की इसी वर्ष आई किताब मेन ऐट होम: इमैजिनिंग लिबरेशन इन कोलोनियल ऐंड पोस्ट-कोलोनियल इंडिया को इसी श्रृंखला की एक जरूरी कड़ी की तरह देखा जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में आई पाण्डेय की इस किताब की जड़ों को उन्हीं के लिखे एक आलेख हिन्दुस्तानी आदमी घर में में खोजा जा सकता है, जो विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सीएसडीएस) से निकलने वाली समाजविज्ञान की ख्यात पत्रिका प्रतिमान के जनवरी-जून, 2018 अंक में छपा था। यद्यपि पाण्डेय का कहना है कि इस विषय में उनकी रुचि कोई नयी नहीं है, लेकिन प्रतिमान में छपे अपने उस आलेख से ही उन्होंने इस क्षेत्र में औपचारिक विषय-प्रवेश किया था।
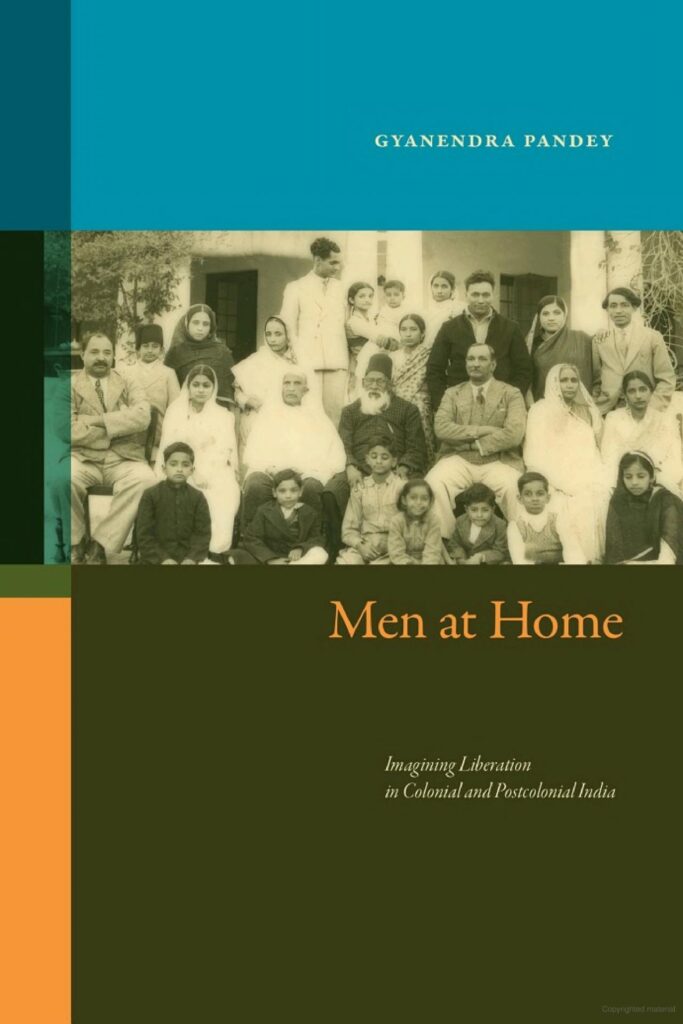
यह तथ्य भी काफी दिलचस्प है कि जिस विषय पर लिखने का आरम्भ लेखक ने हिंदी में किया, जब उसी विषय को सात साल बाद किताब की शक्ल में लाया गया तो उसकी भाषा अंग्रेजी हो गई। अब अपनी ही किताब का हिंदी रूपांतरण खुद पाण्डेय कर रहे हैं, जो अगले साल तक राजकमल प्रकाशन से आने वाला है। इसी तरह, मूलतः हिंदी पट्टी से ताल्लुक रखने वाली अंग्रेजी में छपी इस किताब की शायद यह पहली समीक्षा है जो हिंदी में लिखी जा रही है।
बहरहाल, प्रतिमान में 2018 में छपे अपने आलेख में पाण्डेय ने तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों (मर्दों)- राहुल सांकृत्यायन, मुंशी प्रेमचन्द और राजेन्द्र प्रसाद- के वैवाहिक जीवन को केंद्र में रखकर यह देखने की कोशिश की थी कि जो मर्द अच्छी सामाजिक हैसियत हासिल किए हुए हैं, जो अपने विचारों में अक्सर प्रगतिशील रहे और जो आज तक प्रासंगिक बने हुए हैं, अपने घर में उनकी भूमिका क्या रही है। दूसरे शब्दों में, अगर टैगोर से उनकी शब्दावली उधार लेकर कहें तो, पाण्डेय ने यह देखने की कोशिश की है कि वे मर्द जो सामाजिक जीवन (बाहर) में काफी प्रगतिशील मालूम पड़ते हैं, उनका खुद के निजी जीवन (घर) में व्यवहार कैसा होता है। घरे-बाइरे की यह बाइनरी दो किस्म की सच्चाइयों को जन्म देती है: एक जो दुनिया को दिखती है और दूसरी जो निजी स्पेस में करीबी लोगों (खासकर औरतों) को दिखलाई पड़ती है।
इन सच्चाइयों को उजागर करने के लिए पाण्डेय आत्मकथा की विधा को लेते हैं और उसका मूल्यांकन एक मंझे हुए इतिहासकार की भांति करते हैं। आत्मकथा जैसी विधा को ऐतिहासिक आर्काइव की तरह बरतने की कोशिश इतिहास के अनुशीलन में तुलनात्मक रूप से नई चीज है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि पाण्डेय की ताजा किताब इस चलन को आगे बढ़ाएगी तथा नए शोधार्थियों को इस दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करेगी।
अपनी नयी किताब में पाण्डेय ने प्रतिमान के आलेख वाले तीन मर्दों के अलावा कई और लोगों को शामिल किया है और मर्दों के घरेलू व्यवहार को एक अधिक समावेशी खांचे में देखने की कोशिश की है। जैसा कि पाण्डेय स्वयं भी बताते हैं, कि यह नयी “किताब दक्षिण एशियाई घरेलू दुनिया में मर्दों के अस्तित्व पर एक बड़े निबन्ध जैसी है” (पृ. 1)। किताब इस ओर इशारा करती है कि मर्द अकसर घरेलू अर्थों में मुक्ति को जिस तरह परिभाषित करते हैं, बाहरी दुनिया यानी सार्वजनिक जीवन में उनकी मुक्ति की परिभाषा काफी विरोधाभासी होती है। किताब का केन्द्रीय विषय यह है कि घरेलू हलके में मर्दों का व्यवहार कैसा होता है और कैसे यह व्यवहार अकसर बाहरी दुनिया के उनके आदर्शों के खिलाफ खड़ा पाया जाता है। एक ओर तो ये विभूतियां (वर्णित ऐतिहासिक किरदार) हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कराने का प्रण लिए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अपने घर में उनका व्यवहार कम से कमतर प्रगतिशील है। घरेलू स्पेस में इस खास किस्म के मर्दाना व्यवहार की विशेषता यह है कि वह भारतीय समाज में असमानता की जड़- जाति व्यवस्था- को भी बाइपास कर जाता है और जातिगत पहचानों से पार जाकर मर्दवादी एकजुटता कायम करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है।
हिन्दुस्तानी-आदमी-घर-में-तब-और-अब
किताब मूलतः हिंदीभाषी उत्तर भारतीय विभूतियों पर केन्द्रित है, लेकिन इसमें डॉ. अंबेडकर जैसे चरित्रों को भी लिया गया है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुषों को एक साथ जोड़कर रखने वाला एक धागा है, जिसे पाण्डेय ‘हज्बैंडनेस’ कहते हैं। यह बेहद दिलचस्प परिकल्पना है क्योंकि अमूमन पुरुषों को “औरतों की भांति उनके अस्तित्व के किसी एकल आयाम तक सीमित नहीं किया जाता है” (पृ. 6)। औरतों का तो पूरा जीवन ही घर के शाश्वत ढांचे के इर्द-गिर्द बुना हुआ होता है, लेकिन मर्दों के जीवन में यह ढांचा सबसे कम अहमियत रखते हुए भी उनके जीवन को गढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किताब इसी दुविधा के इर्द-गिर्द घूमती है। लेखक का दावा है कि यह किताब “साधारण लोगों के साधारण जीवन की एक कहानी है, जिसे घरेलू नजरिये से कहा गया है” (पृ. 8)।
अपनी शख्सियत को गढ़ने में मर्द अपने घर पर कितना अधिक निर्भर होते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए नारीवादी घेरों में चलने वाली एक उक्ति ही काफी है, जो कहती है कि ‘’अगर औरतों के श्रम का हिसाब होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी’’। घरेलू दुनिया पर इस निर्भरता के बावजूद, मर्दों की अपने घर में बतौर पति, पिता या पुत्र कितनी उपस्थिति रहती है इस पर कई अध्ययन हो चुके हैं और सभी अध्ययन कमोबेश यही सुझाते हैं कि अधिकतर मर्द इन सभी भूमिकाओं को निभाने में नाकाम साबित होते हैं। इसका एक उदाहरण बच्चों की परवरिश के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसको लेकर चालू संस्कृति में आजकल ‘ऐब्सेंट फादर’ (अनुपस्थित पिता) जैसे शब्द प्रचलन में आ चुके हैं।
ज्ञानेंद्र पाण्डेय की किताब तीन भाग में विभाजित है। आगे जाकर ये तीन भाग कुल सात अध्यायों में विभक्त हैं। इसके अलावा, एक प्रस्तावना और एक उपसंहार भी है। यहां हम इन अध्यायों की विषयवस्तु में गहरे न जाकर यह काम पाठकों के लिए छोड़ रहे हैं, मगर कुछ मोटी बातें बता देना जरूरी है। पहले भाग में दो अध्याय हैं जो हमें भारतीय मर्दों के ‘स्व’ की बुनावट को समझाने का प्रयास करते हैं। इस भाग में लेखक एक घरेलू जगह के रूप में ‘घर’ का बेहद दिलचस्प विवरण पेश करते हैं; ऐसा लगता है कि इन महान विभूतियों के घरों में वे टहल रहे हैं। इसके अलावा लेखक बचपन को बतौर माध्यम इस्तेमाल करते हैं और कुछ हद तक मनोविश्लेषण वाले अंदाज में बतौर वयस्क इन मर्दों की बुनावट को समझने का प्रयास करते हैं। अगले भाग में कर्तव्य, अनुशासन और सम्मान जैसे जुमलों के माध्यम से लेखक इन शब्दों के द्विअर्थी मायनों को समझाने की कोशिश करते हैं; वे बताते हैं कि कैसे इन शब्दों के अर्थ घर और बाहर की दुनिया में अलग-अलग हो सकते हैं।
यहां यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे ‘कर्तव्य’ जैसी चीजें मर्दों के लिए एक हथियार बन जाती हैं और वे ‘देशप्रेम’ आदि के नाम पर अपने घर, खासकर औरतों, को छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह जाने-अनजाने एक मर्दवादी समाज में रहने के नाते कुछ विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका उन्हें जरा भी भान नहीं होता। शायद इसीलिए पाण्डेय इन्हें “अधिकतर घर में रहने के बावजूद घर से दूर” बतलाते हैं (पृ. 82), हालांकि यहां घर से दूर होने का आशय वैरागी राष्ट्रवादियों की तरह पूरी तरह गृहत्याग नहीं है। इस सवाल को समझाते हुए पाण्डेय ‘घरे-बाइरे’ की लैंगिक समझ, यानि औरतें घर संभालें और मर्द दुनिया, को भी चुनौती देते हैं और इस विरोधाभास को खोलते हैं कि कैसे मर्द हमेशा ही “परिवार, घर, औरतों, नौकरों, और अन्य सहायकों पर निर्भर रहते हैं ताकि वे अपने ‘सामाजिक कामों’ को कर सकें” (पृ. 83)।
इसके बाद पाण्डेय हमारा ध्यान उस पेशेवर मध्यवर्ग की ओर खींचते हैं जो विभाजन और आजादी के दौरान अस्तित्व में आया। पाण्डेय के अनुसार, यह नया मध्यवर्ग “पूरी तरह औरतों और पुरुषों से जुड़ी नैसर्गिक भूमिकाओं के बारे में अपनी पारम्परिक समझदारी से बाहर नहीं आ सका था” (पृ. 109) और इस वजह से ‘घर’ और ‘बाहर’ के बीच का लैंगिक विभाजन ज्यों का त्यों बना रहा। इस तरह “स्वतन्त्रता और अनुशासन के बीच की यह विरोधाभासी कुश्ती जारी रही” जिसने घरेलू एवं सार्वजनिक जगहों के बंटवारे में अलग-अलग रूपों में आधुनिक परिवारों को प्रभावित किया (पृ. 110)।
इसके बाद पाण्डेय भारतीय समाज में जाति जैसी अनिवार्य परिघटना की ओर जेंडर की निगाह से हमारा ध्यान खींचते हैं और दलितों के दृढ़कथन (असर्शन) में निहित लैंगिक आयामों और कमी-कमजोरियों को रेखांकित करते हैं। यहां हमें यह देखने को मिलता है कि जाति जैसी कठोर संरचना भी “आधुनिक पितृसत्ता के दोबारा सुदृढ़ीकरण” के माध्यम से मर्दों के लिए सहूलियत पैदा करती है। शायद यही वह बिंदु है जहां चारु गुप्ता द्वारा प्रतिपादित दलित मर्दानगी वाली अवधारणा को जोड़ा जा सकता है।
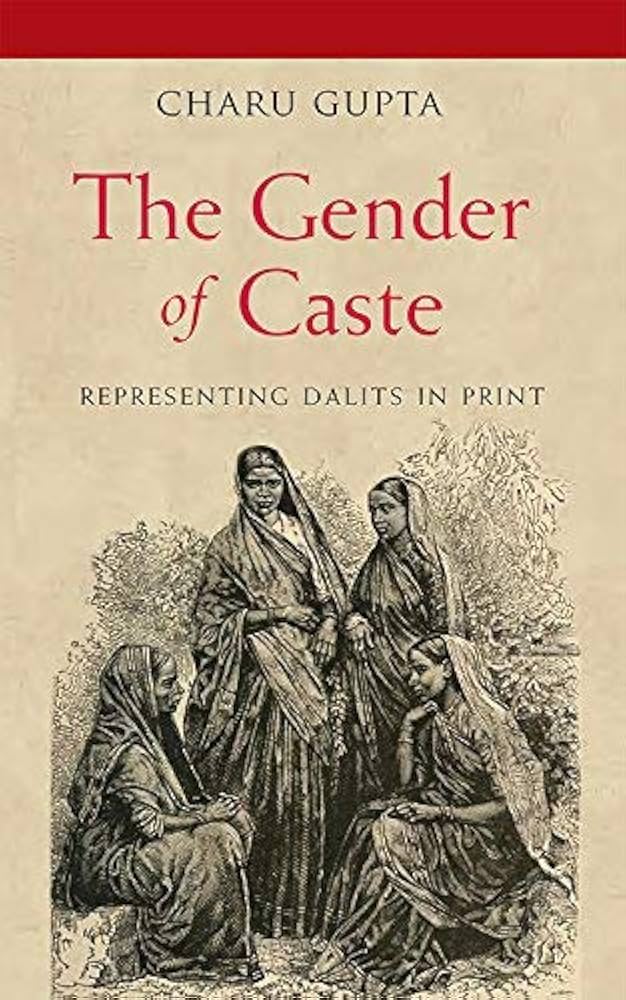
किताब के तीसरे भाग में पुरुषत्व के सांस्कृतिक आयामों की ओर ध्यान दिलाया गया है- विशेष रूप से जाति और वर्ग जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। इन्हीं को केंद्र में रखकर (उच्च-जाति के) पुरुषों द्वारा कुछ कार्यों को करने, जैसे सफाई, में मौजूद हिचक और उसके पीछे की सोच-समझ का विश्लेषण किया गया है (पृ. 137)। यहां पाण्डेय भिन्न सांस्कृतिक आयामों के बीच मर्दों में मौजूद परस्पर कटावों की ओर इशारा करते नजर आते हैं। यह हमें बताता है कि जेंडर के संदर्भ में किसी भी ढांचे का विश्लेषण करने के लिए सांस्कृतिक आयामों की प्रतिच्छेदी अवधारणा एक औजार के रूप में कितनी अहम है।
मर्दानगी भी एक ऐसी ही संरचना है जो कई स्तरों पर एक ओर तो ‘भाईचारा’ जैसा कुछ पैदा करती है (जिसे आजकल ब्रो-कोड कहते हैं), लेकिन कई दूसरे मौकों पर अन्य सामाजिक संरचनाओं के प्रभावों की वजह से भेदभाव को भी जनती है। अंतिम अध्याय में पाण्डेय यह दिखाते हैं औरतों के बारे में और स्वयं के बारे में मर्द क्या सोचते हैं और किस तरह से उनकी यह सोच उनके घरेलू और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित और प्रभावित करती है।
बहुलता के स्थान पर एकाश्म को तवज्जो देने के अपने खतरे होते हैं, बावजूद इसके पाण्डेय ने इस किताब के माध्यम से लैंगिकता और मर्दानगी पर हो रहे वर्तमान शोधों में एक अहम योगदान दिया है। इस किताब की सबसे दिलचस्प और खास बात मूल स्रोतों के रूप में आत्मकथा सरीखी विधा का चयन है। किताब में मौजूद आख्यानों के माध्यम से हमें पुरुषत्व और जेंडर को उनमें मौजूद विरोधाभासों के साथ और गहरे ढंग से समझने का मौका मिलता है। जेंडर से जुड़े किसी भी क्षेत्र में काम करे शोधार्थियों, अध्येताओं आदि के लिए यह किताब एक कारगर दस्तावेज हो सकती है।
भाषाई अनुवाद के स्तर पर पाण्डेय ने कुछ बड़े दावे किए हैं जिनसे हिंदी के विद्वान शायद असहमति रखें, लेकिन उम्मीद है कि जब वे किताब का हिंदी में रूपांतरण करेंगे तब शायद उन्हें उन दावों से कुछ निजात मिल सकेगी।
पुस्तक समीक्षा: मेन ऐट होम: इमैजिनिंग लिबरेशन इन कोलोनियल ऐंड पोस्ट-कोलोनियल इंडिया, ज्ञानेंद्र पाण्डेय (2025), ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम एवं लन्दन







