पिछले दिनों गार्डियन अखबार की दो साल पुरानी एक रिपोर्ट हैज़ इंडिया लॉस्ट इट्स सेंस ऑफ़ ह्यूमर? पर नजर पड़ गई। उसमें बताया गया था कि भारत की सार्वजनिक और राजनीतिक संस्कृति धीरे-धीरे हास्य-विनोद, व्यंग्य और आत्म-विडंबना को सहन करने की क्षमता खोती जा रही है। इसके पीछे विपक्ष के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर हुए विवाद का उदाहरण दिया गया था। उस रिपोर्ट में ऐसे स्टैंड-अप कॉमेडियन, कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकारों के उदाहरण भी दिए गए हैं जिनमें से किसी को जेल हुई, किसी की नौकरी चली गई, तो कई को अनौपचारिक सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। बहरहाल, उस रिपोर्ट ने लगभग दो दशक पुरानी एक मुलाकात की याद दिला दी।
दिल्ली के कटवारिया सराय बाजार में आज जहां हल्दीराम है वहीं कभी एक रेस्टोबार हुआ करता था मैंडरिन कोर्ट। दिवंगत पत्रकार प्रफुल्ल बिदवई, प्रोफेसर अचिन वनाइक, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने वाली संस्था ‘पीस’ के चीफ एक्जीक्यूटिव और दिवंगत शिक्षाविद् अनिल चौधरी के साथ मैं भी मैंडरिन कोर्ट के खानपान का आनंद ले रहा था। बातचीत कई विषयों से घूमते हुए ‘इंडियन सोसायटी में ह्यूमर’ पर आ गई। ह्यूमर यानी हास्य-विनोद पर बात पहली नजर में तो पूरे भारतीय समाज के संदर्भ में थी, लेकिन लगा यह कि चर्चा का जोर हिंदीभाषी क्षेत्रों पर है। प्रो. वनाइक का कहना था कि भारत में ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ नहीं के बराबर है।
तब मैंने बीरबल, तेनालीराम और गोनू झा का जिक्र किया। ऐसा नहीं रहा होगा कि अचिन वनाइक जैसे बुद्धिजीवी को अलग-अलग भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों से आने वाले और भारतीय लोक-स्मृति में रचे-बसे बीरबल, तेनालीराम और गोनू झा जैसे नाम मालूम नहीं हों, जो व्यंग्य, बुद्धि और सत्ता-समीक्षा की दीर्घ परंपरा के प्रतिनिधि हैं। इन तीनों की भूमिका एक जैसी है- राजा, सत्ता और समाज को हँसते-हँसते आईना दिखाना। बहरहाल, बातों ने फिर अलग मोड़ ले लिया और हम दूसरी बातों में मशगूल हो गए, पर मेरे दिमाग में ये तीनों नाम देर तक गूंजते रहे थे।

जहां तक भारतीय समाज में ह्यूमर के न होने की बात कही जाती है, अगर तथ्यों पर जाएं तो स्थिति कमजोर नहीं दिखती। भारत के लोकवृत्त में हास्य की परंपरा प्राचीन काल से ही विकसित होती दिखती है, जो बीरबल, गोनू झा और तेनालीराम जैसे व्यक्तित्वों के माध्यम से मनोरंजन, नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यंग्य का स्थायी माध्यम बनी। यह परंपरा आज भी साहित्य, फिल्मों और लोककथाओं में जीवित है और दर्शाती है कि हास्य केवल हँसी नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब भी हो सकता है। यह परंपरा केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक संदेशों को सहज रूप में प्रसारित करने का माध्यम भी रही है। लोकवृत्त में हास्य का इतिहास कई दृष्टियों से देखा जा सकता है, जिनमें सत्ता, राजनीति से लेकर साहित्य एवं सिनेमा जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
राजनीति में हास्य-विनोद
राजनीति के क्षेत्र में देखें, तो 1950 और 1960 के दशक में जब हमारी संसद युवा थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू, पीलू मोदी, राम मनोहर लोहिया जैसे कद्दावर थे, ये लोग कटु टिप्पणियों और तीखे शब्दों को आसानी से संभाल लेते थे।
एक बार लोहिया ने सदन में नेहरू के बारे में कहा था कि ‘‘वे कुलीन नहीं हैं।‘’ लोहिया ने कहा था, “मैं साबित कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री के दादा मुगल दरबार में चपरासी थे।” इसके जवाब में नेहरू मुस्कुराए और बोले, “मैं खुश हूं कि माननीय सदस्य ने आखिरकार वो स्वीकार कर लिया है जो मैं उन्हें इतने वर्षों से समझा रहा हूं कि मैं जनता का आदमी हूं।” इस अप्रत्याशित मौके पर एक भी कांग्रेसी ने खड़े होकर शेम, शेम चिल्लाते हुए ऐसा नहीं कहा था कि “तुमने हमारे नेता को चपरासी का पोता कहा।”
एक अन्य अवसर पर स्वतंत्र पार्टी के नेता पीलू मोदी को स्पीकर की ओर पीठ करके बात करने के कारण आसन की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया। गोलमटोल दिखने वाले पीलू मोदी ने खुद को बचाते हुए कहा था, “सर, मेरे पास न तो फ्रंट है और न बैक, मैं गोल हूं।”
अपने ऊपर ही हँसने और व्यंग्य करने वाली ऐसी टिप्पणियां आज दुर्लभ हैं। आज मजाक करना खतरनाक हो गया है क्योंकि हास्य हमेशा से ही असहमति का एक मजबूत औजार रहा है। कुछ भारतीयों का मानना है कि मौजूदा सरकार के दौर में देश की राजनीतिक हास्य क्षमता ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत में ब्रिटेन की ‘प्राइवेट आइ’ या फ्रांस की ‘चार्ली हेब्दो’ या ‘ल कैनार्ड इनचेन’ जैसी कोई प्रभावशाली व्यंग्यात्मक पत्रिका भी नहीं है, न ही अमेरिका की तरह यहां व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर (अमेरिकी व्हाइट हाउस संवाददाताओं के संघ WHCA द्वारा आयोजित एक वार्षिक समारोह) जैसा कोई आयोजन होता है जिसमें राष्ट्रपति आमतौर पर भाग लेते हैं और हास्यपूर्ण भाषण देते हैं।
साहित्य में हास्य-व्यंग्य
मुग़ल साम्राज्य के अवसान और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साक्षी महान शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ाँ ग़ालिब (1797–1869) का हास्यबोध एक टूटते हुए संसार की बौद्धिक प्रतिक्रिया था। वह हल्का-फुल्का मनोरंजन या मसख़री नहीं था, बल्कि विडंबना, आत्म-व्यंग्य और ऐतिहासिक त्रासदी की समझ से उपजा ह्यूमर था।
1857 के बाद दिल्ली उजड़ चुकी थी। दोस्त मारे गए, संरक्षक खत्म हो गया, शायर बेसहारा रह गया। ग़ालिब इसे करुण क्रंदन में नहीं, व्यंग्यात्मक ठंडेपन में लिखते हैं, “अंग्रेज़ों ने दिल्ली की हवा इतनी साफ़ कर दी कि अब सांस लेना भी ग़ैर-मुल्की लगता है।” यह औपनिवेशिक आधुनिकता पर कटाक्ष है जहां साफ़-सफ़ाई तो है, लेकिन आत्मा नष्ट हो चुकी है। ग़ालिब का हास्य उस ऐतिहासिक संक्रमण के दौर की पतनशील सभ्यता की बुद्धिमान हँसी थी। वह हँसी एक बुद्धिजीवी की बेबसी भी थी।

उर्दू साहित्य में हास्य-विनोद की पुरानी परंपरा रही है। इसी वजह से उर्दू के महान रचनाकारों के बारे में आम लोगों के बीच बहुत से लतीफे प्रचलित हैं। मीर, ग़ालिब के शेरों और उनके रोचक प्रसंगों से आम लोग भी वाकिफ हैं। हिंदी साहित्य में भी हास्य-विनोद कई माध्यमों से सामाजिक कुरीतियों, मानवीय कमजोरियों और जीवन की एब्सर्डिटी पर कटाक्ष करता है। यह चुटकुलों, लतीफों, और व्यंग्यात्मक कहानियों के रूप में प्रकट होता है, जहां पंचलाइन या अंतिम वाक्य हास्य पैदा करता है।
मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी (प्रभुलाल गर्ग) के कटाक्ष की बानगी देखिए, जिन्होंने 1932 में ‘संगीत कार्यालय हाथरस’ स्थापित किया, जो हास्य कविता का केंद्र बना। उनकी व्यंग्यपूर्ण रचनाएं सामाजिक कुरीतियों पर वार करते हुए हास्य पैदा करती हैं:
नेता अखरोट से बोले किसमिस लाल
हुज़ूर हल कीजिए मेरा एक सवाल
मेरा एक सवाल, समझ में बात न भरती
मुर्ग़ी अंडे के ऊपर क्यों बैठा करती
नेता ने कहा, प्रबंध शीघ्र ही करवा देंगे
मुर्ग़ी के कमरे में एक कुर्सी डलवा देंगे
हिंदी ही नहीं, बल्कि सारी भाषाओं में साहित्यकारों की जिन्दगी से जुड़े कई दिलचस्प विनोद प्रसंग मिलते हैं। इन प्रसंगों से गंभीर दिखने वाले रचनाकारों की भी एक सहज छवि बनती है। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पत्रिका ‘सरस्वती’ में संपादक श्रीनारायण चतुर्वेदी ने महान साहित्यकारों के ऐसे रोचक और मनोरंजक संस्मरणों की एक पूरी शृंखला प्रकाशित की थी।
एक किस्सा मैथिलीशरण गुप्त के सार्वजनिक “राष्ट्रकवि” व्यक्तित्व और उनके निजी मानवीय स्वभाव के बीच के अंतर को अत्यंत चुटीले ढंग से उघाड़ता है। राय कृष्णदास- जो स्वयं एक कलारसिक, उदार और ‘बुंदेलखंडी ठसक’ वाले साहित्यप्रेमी थे- द्राक्षासव (अंगूर की शराब) की बोतल लेकर गुप्तजी से मिलने पहुंचे। गुप्तजी उस समय घर पर नहीं थे। राय साहब प्रतीक्षा करते रहे, अंततः चले गए, और खाली बोतल वहीं छोड़ गए। जब मैथिलीशरण गुप्त लौटे और मेज़ पर बोतल देखी, तो क्षण भर के लिए उनका मन प्रसन्न हुआ— पर जैसे ही पता चला कि वह खाली है, उनका ‘राष्ट्रकवि’ मन नहीं, बल्कि मनुष्य मैथिलीशरण आहत हो गया। उसी क्षण उन्होंने क्रोध और व्यंग्य में एक कविता लिखी, जो आगे चलकर साहित्यिक किस्सा बन गई।
वह कविता कुछ इस प्रकार थी:
कृष्णदास! यह करतूत किस क्रूर की?
आए थके हारे हम यात्रा कर दूर की।
द्राक्षासव तो न मिला, बोतल ही रीती थी!
जानते हमीं हैं तब हम पर जो बीती थी!
ऐसी घड़ी भी हा! पड़ी उस दिन देखनी-
धार बिना जैसे असि, मसि बिना लेखनी!
इस कविता में एक युग का सांस्कृतिक द्वंद्व छिपा है। मैथिलीशरण गुप्त सार्वजनिक रूप से सात्विकता आदि के कवि माने जाते थे। राय कृष्णदास का खाली बोतल छोड़ जाना और गुप्तजी का उस पर कविता लिख देना, यह दिखाता है कि हिंदी नवजागरण के महानायक भी भीतर से ग़ालिब की तरह ही मनुष्य थे- हँसने और चिढ़ने-चिढ़ाने वाले।
प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। एक बार परसाई जी के घर उनके एक मित्र आए और पीने के लिए जिन की मांग कर दी। परसाई जी ने कहा कि घर में देख लो, कहीं मिल जाएगी। काफी ढूंढने पर भी दोस्त को जिन नहीं मिली। फिर परसाई जी उठे और दूर रखी आलमारी की बगल में जाकर ढूंढने लगे कि अचानक बोल पड़े– ‘जिन’ ढूंढा, ‘रम’ पाइयाँ’। और इस तरह परसाई जी ने कबीरदास की प्रसिद्ध साखी “जिन खोजा तिन पाइयाँ” की दिलचस्प पैरोडी रच दी।
दो किस्से और देखिए। एक किस्सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से और दूसरा उनके शिष्य प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह से जुड़ा है। पहला किस्सा। सौंदर्यशास्त्र के विद्वान लेखक रमेश कुंतल मेघ के बारे में प्रचलित है कि उनकी भाषा अत्यंत क्लिष्ट रही है। हुआ यह कि एक बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमेश कुंतल मेघ का आमना-सामना हो गया। औपचारिक बातचीत के बाद मस्तमौला द्विवेदी जी ने कहा– ‘‘डॉ. साहब, अब तो आपकी किताबों का भी हिंदी अनुवाद आ जाना चाहिए।’’
एक जमाने की मशहूर पत्रिका ‘धर्मयुग’ ने हिंदी साहित्यकारों पर हास्यपूर्ण चुटकुलों और प्रहसनों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जो साहित्यिक व्यक्तित्वों की विशेषताओं पर तीखा और नरम तंज भी करती थी। ‘धर्मयुग’ के ये चुटकुले 1960-70 के दशक में लोकप्रिय हुए, जो साहित्यकारों की छवि को हल्के-फुल्के ढंग से उकेरते थे। देखिए:
दिल्ली में सड़कों पर नई-नई ट्रैफिक लाइटें लगी ही थीं। एक व्यक्ति लाइट के साथ अपनी दिशा बदल लेता था। कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ जाता था। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने उसकी गतिविधि को देखकर कहा, ‘ऐ धोती वाले बाबा, तुम कभी दाएं तो कभी बाएं क्यों जाते हो?’ वहीं दो लेखक भी पास में खड़े थे। दोनों ने छूटते ही एक साथ कहा, ‘यह पुलिसवाला नामवर जी की आलोचना को कितनी अच्छी तरह से समझता है।’
नामवर सिंह जैसे आलोचक के संदर्भ में यह चुटकुला उनकी आलोचना शैली की जटिलता और परिवर्तनशीलता को रेखांकित करता है और उनकी बौद्धिक चपलता पर हास्यपूर्ण टिप्पणी करता है। नामवर सिंह (1926-2019) हिंदी के प्रमुख आलोचक थे, जिनकी पुस्तक ‘कविता के नए प्रतिमान’ ने साहित्य जगत को प्रभावित किया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 से प्रकाशित अपनी पत्रिका ‘हरिश्चंद्र चंद्रिका’ (जिसे श्रीहरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहा जाता है) में व्यंग्यात्मक रचनाओं, मुकरियों और हास्यपूर्ण चुटकुलों को जगह दी, जो उस युग की सामाजिक-राजनीतिक विसंगतियों पर कटाक्ष करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध मुकरी “भीतर भीतर सब रस चूसे” उनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हास्यपूर्ण रचनाओं का उदाहरण है। यह पंक्ति तत्कालीन लोकप्रिय मुकरियों (हास्य-प्रधान पहेलियाँ या चुटकुले) की शैली को दर्शाती है, जो बौद्धिक कौशल की परीक्षा लेती थीं। हरिश्चंद्र चंद्रिका में ऐसी मुकरियाँ नवजागरण काल में जनता को आकर्षित करने और जागृति फैलाने के लिए छापी जाती थीं। भारतेंदु ने ऐसी 14 मुकरियाँ रचीं, जो हिंदी नवजागरण की व्यंग्य शैली का प्रतीक हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध मुकरी “भीतर भीतर सब रस चूसे” उनके “नये जमाने की मुकरियाँ” संग्रह में शामिल है, जो ब्रिटिश शासनकाल के छलपूर्ण शोषण पर तीखा व्यंग्य करती है। यह दो सखियों के संवाद रूप में रची गई है, जिसमें अंग्रेजों की चालाकी और लूट को रसभरे एवं हास्यपूर्ण ढंग से उजागर किया गया है।
भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसि हंसि के तन मन धन मूंसे।
जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि साजन? नहिं अंग्रेज।
एक सखी दूसरी से पूछती है कि वह कौन है जो छल से सब कुछ लूट रहा है, मीठी बातों से सब हड़प लेता है और बातचीत में तेज है। वह पूछती है कि क्या यह साजन है, तो दूसरी सखी भारत का संदर्भ लेते हुए उत्तर देती है- साजन नहीं, यह अंग्रेज है। यह मुकरी औपनिवेशिक शोषण के बारे में लोगों को जागृत करती है, जहां अंग्रेज व्यापार के बहाने देश को खोखला कर रहे थे।
सिनेमा में कॉमेडी
हँसी सामाजिक तनावों का विसर्जन भी है और कभी-कभी प्रभुत्वशाली व्यवस्था के लिए एक ‘सेफ़्टी वॉल्व’ भी। यह सिनेमा में कॉमेडी के रूप में साफ दिखता है।
हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन का होना केवल एक सिनेमाई या सौंदर्यगत प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सत्ता, वर्ग, बाजार और संस्कृति के अंतर्संबंधों से जुड़ा हुआ एक गहन वैचारिक प्रश्न है। भारतीय सिनेमा के लगभग सौ वर्षों के इतिहास में कॉमेडी फिल्में शुरू से ही एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। समय के साथ ये फ़िल्में विभिन्न रूपों में विकसित होती गईं- जैसे स्लैपस्टिक यानी देह-आधारित कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, प्रहसन, व्यंग्य, डार्क कॉमेडी- और हाल के वर्षों में अपने ‘बॉलीवुडकृत’ अवतार में यह कॉमेडी करोड़ों रुपये के बॉक्स-ऑफिस क्लब तक पहुंचने में भी सफल रहीं।
संस्कृति केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचारधारा का वाहक होती है। ग्राम्शी के ‘हेजेमनी’ के सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी सत्ता को केवल बल से नहीं, बल्कि सहमति के निर्माण से कायम रखता है। हिंदी सिनेमा का कॉमेडियन इसी सहमति-निर्माण की प्रक्रिया में एक जटिल भूमिका निभाता था- वह व्यवस्था पर हँसता भी था और उसी व्यवस्था को सहनीय भी बनाता था।
शिक्षाविद्, शोधकर्ता और संचार व मीडिया अध्येता डॉ. मैथिली गंजू बॉलीवुड को गढ़ने में कॉमेडी फिल्मों की भूमिका पर किए अपने अध्ययन में कहती हैं- “बॉलीवुड में हास्य कॉमिक रिलीफ के जरिये सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करता है।” डॉ. गंजू के अनुसार, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में कॉमेडी फिल्में उत्तर-उदारीकरण (पोस्ट-लिबरलाइज़ेशन) दौर के ‘बॉलीवुड’ स्वरूप में एक स्वतंत्र और सशक्त विधा (जॉनर) के रूप में उभरकर सामने आई हैं। यह परिवर्तन कॉमेडी फिल्मों के निर्माण, वितरण और उपभोग (कनजम्पशन) के स्तर पर आए एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है। आनंद की तलाश और ‘फ़ील-गुड’ अनुभव के साथ कॉमेडी फिल्में देखने की प्रवृत्ति ने एक विशिष्ट कॉमेडी दर्शक-वर्ग को जन्म दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कॉमेडी विधा न केवल बॉलीवुड में, बल्कि टेलीविजन, विज्ञापनों, डिजिटल माध्यमों और हाल के वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर भी एक पसंदीदा मनोरंजन के फॉर्मेट के तौर पर उभरकर सामने आई है।

सिनेमाई पर्दे पर हास्यबोध की बात हो तो 1983 की केतन मेहता की फिल्म ‘जाने भी दो यारों’ पर खास ध्यान चला जाता है। इस फिल्म के हास्यबोध ने हिन्दी सिनेमा में कॉमेडी को देखने की दृष्टि को मूल रूप से बदल दिया था। यह केवल एक हास्य-फिल्म नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यंग्य और नैतिक हस्तक्षेप की सशक्त मिसाल है। इस फिल्म के संदर्भ में हिन्दी सिनेमा की कॉमेडी को एक ऐसे माध्यम के रूप में समझा जा सकता है, जो मनोरंजन के साथ-साथ सत्ता, व्यवस्था और सामाजिक पाखंड को उजागर करता है। हिन्दी सिनेमा की मुख्यधारा कॉमेडी परंपरागत रूप से “रिलीफ़” का कार्य करती रही है- यानी गंभीर कथा के बीच दर्शकों को हँसाकर तनाव कम करना। इसके विपरीत ‘जाने भी दो यारों’ की कॉमेडी कथा के हाशिये पर नहीं, बल्कि कथा की आत्मा है। यहां हास्य किसी पात्र की विशेषता नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे की विडंबना से उपजता है। भ्रष्ट बिल्डर, बिकाऊ पत्रकार, अवसरवादी पुलिस और निष्क्रिय नौकरशाही, सभी हास्य के माध्यम से बेनकाब होते हैं।
फिल्म की कॉमेडी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका एब्सर्ड (अतार्किक) ढांचा है। महाभारत के दृश्य का पुनर्पाठ, लाश के साथ भाग-दौड़, अदालत की कार्यवाही का तमाशा- ये सब दृश्य दर्शकों को हँसाते हैं, लेकिन यह हँसी असहज है। यह हँसी इस बोध से आती है कि व्यवस्था इतनी विकृत हो चुकी है कि उसे तर्क से नहीं, केवल अतिशयोक्ति और व्यंग्य से ही समझा जा सकता है। इस अर्थ में ‘जाने भी दो यारों’ भारतीय शहरी मध्यवर्ग की हताशा की सामूहिक अभिव्यक्ति है।
‘जाने भी दो यारों’ यह भी दिखाती है कि हिन्दी सिनेमा में कॉमेडी केवल “लोकप्रिय” या “हल्की” विधा नहीं है। यह सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम बन सकती है, बशर्ते वह सत्ता से समझौता न करे। बाद के वर्षों में मुख्यधारा कॉमेडी ने इस परंपरा को लगभग त्याग दिया और उपभोक्तावादी हास्य की ओर बढ़ गई, जहाँ हँसी सवालों को कुंद करती है। इसके उलट ‘जाने भी दो यारों’ की हँसी सवालों को तेज करती है।
हिंदी सिनेमा के हास्य-अभिनय की परंपरा में एक नाम ‘जॉनी’ का उल्लेख जरूरी लगता है जो केवल एक नाम भर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। यह नाम बार-बार लौटता है- अलग-अलग दशकों में, अलग-अलग सामाजिक संदर्भों में- और हर बार हास्य के माध्यम से अपने समय की सच्चाइयों को उजागर करता है।
जॉनी वॉकर से लेकर जॉनी व्हिस्की और फिर जॉनी लीवर तक, यह यात्रा भारतीय समाज, उसके वर्ग-चरित्र और बदलते जन-स्वाद की यात्रा भी है। हिंदी सिनेमा में ‘जॉनी’ नाम एक हास्य-वंशावली का संकेतक है। यह दिखाता है कि कॉमेडी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है जो हर दौर में अपना रूप बदलती है, पर अपना मूल कार्य नहीं छोड़ती। एक अर्थ में, जॉनी वॉकर की भावुक आत्मीयता, जॉनी व्हिस्की की भद्दी सच्चाई और जॉनी लीवर की व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता- तीनों मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि हिंदी सिनेमाई हास्य का विकास दरअसल भारतीय समाज के आत्मबोध का विकास है।
यह संयोग नहीं है कि इस परंपरा की शुरुआत एक शराबी पात्र से होती है क्योंकि भारतीय सिनेमा में शराबी हमेशा हाशिये पर खड़ा वह व्यक्ति रहा है जो व्यवस्था से बाहर होकर भी सच बोलने का नैतिक अधिकार रखता है। जॉनी वॉकर (बदरुद्दीन जमालुद्दीन काज़ी) की प्रसिद्ध शराबी छवि को अक्सर नैतिक पतन के रूप में देखा गया, लेकिन यह छवि शहरी जीवन की एलियेनेशन की भावना की अभिव्यक्ति थी। जॉनी वॉकर की कॉमेडी सीधे शहरी मेहनतकश वर्ग से निकलती थी। बस-कंडक्टर, शराबी, छोटा कर्मचारी- उनके पात्र पूंजीवादी शहर की असमानताओं को सहज हास्य में बदल देते थे। उनका शराबी पात्र मसखरा नहीं, बल्कि हाशिये का दार्शनिक था जो लड़खड़ाता जरूर था, पर नजरिया स्पष्ट रखता था।

(स्रोत: जॉनी लीवर का इंस्टाग्राम खाता)
सिनेमाई पर्दे पर हास्यबोध ने वैसे तो कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, पर प्रत्येक दौर में हास्य कलाकार प्रमुख नायकों के पूरक होते हैं। नायक का ‘ऑरा’ जितना बड़ा होता गया, सहायक और हास्य पात्र उतने ही सिकुड़ते गए। कॉमेडियन, जो कभी कथा-संरचना का आवश्यक अंग था, अब केवल ‘फिलर’ बन गया। यह केवल सौंदर्य का प्रश्न नहीं, बल्कि श्रम के अवमूल्यन का प्रश्न है। कॉमेडियन का श्रम, टाइमिंग, शारीरिक अभिव्यक्ति, संवाद धीरे-धीरे अदृश्य कर दिया गया। हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन का पतन दरअसल उस वर्गीय और वैचारिक पुनर्संरचना का परिणाम है, जिसमें सिनेमा जन-संस्कृति से हटकर पूंजी-केन्द्रित मनोरंजन उद्योग में बदल गया। सवाल किया जा सकता है कि हँसी कैसे वर्गीय अनुभव से निकलती है? कैसे वह ‘हेजेमनी’ का उपकरण भी बन सकती है? और कैसे नव-उदारवाद में उसका वस्तुकरण (कमोडिफिकेशन) हो गया?
हिंदी सिनेमा में हीरो द्वारा कॉमेडियन की भूमिका निभाना केवल अभिनय की शैली का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक-सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारतीय समाज में हास्य, सत्ता, वर्ग और लोकप्रियता के संबंध समय के साथ कैसे बदले हैं। कहा जा सकता है कि नव-उदारवादी दौर में हँसी का वस्तुकरण हो गया है, वह एक वस्तु बन गई। पंचलाइन, मीम और वायरल क्लिप- ये सब हँसी को क्षणिक उपभोग में बदल देते हैं। ऐसे में चरित्र-आधारित कॉमेडी, जो समय और धैर्य मांगती है, अनुपयोगी मानी जाती है। यह प्रक्रिया कॉमेडियन को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे ‘कंटेंट-प्रोड्यूसर’ में बदल देती है।
इसके लिए क्या दर्शक दोषी हैं? दर्शकों को भी पूरी तरह स्वायत्त नहीं माना जा सकता। उनकी पसंद भी उसी वैचारिक ढांचे में निर्मित होती है जिसमें वे रहते हैं। इसलिए हिंदी सिनेमा से कॉमेडियन के गायब होने का दोष केवल दर्शकों पर डालना संरचनात्मक कारणों से ध्यान हटाने जैसा होगा।
राजा और धर्म का उपहास
इस लेख को लिखते वक्त जब मैं इसके बारे में अभिषेक श्रीवास्तव से चर्चा कर रहा था तो दो नई जानकारी मिली– एक ज़ाफ़र ज़टल्ली के बारे में और दूसरा क्षेमेन्द्र के बारे में। यह जानकारी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है।
ज़ाफ़र ज़टल्ली को उर्दू का “पहला व्यवस्थित तंज़–मज़ाह शायर” कहा जाता है, जिन्होंने हज्व (निंदा, आलोचना या व्यंग्यपूर्ण तिरस्कार में रची गई कविता) को व्यक्तिगत दुश्मनी से सामाजिक–राजनीतिक आलोचना तक विस्तार दिया; लेकिन उनकी फहाशत (अश्लीलता) ने उन्हें “पोर्नोग्राफ़र” जैसी छवि दे दी। अकबर इलाहाबादी (1846–1921) ने भी ब्रिटिश राज, पश्चिमी शिक्षा, मुस्लिम नकल पर हास्य–व्यंग्य किया; उनका हज्व “लिसान–उल–अस्र” (युग का स्वर) बना, लेकिन उन्होंने ज़टल्ली की तरह मौत का खतरा नहीं उठाया।
मुग़ल सम्राट फ़र्रुख़सियर ने जाफ़र ज़टल्ली को बग़ावत/बे–अदबी भरे कलाम की वजह से मौत की सज़ा दी। उर्दू स्रोतों में दर्ज है कि 1716 के आसपास उन्हें जूते के तस्मे से गला घोंट कर मार डाला गया। एक मशहूर बात यह है कि उन्होंने फ़र्रुख़सियर की तख़्त–नशीनी पर वह व्यंग्यात्मक मिसरा लिखा था जिसमें इशारा था कि ख़ज़ाना खाली है और बादशाह “तस्मा–कश” (यानी लोगों का गला तस्मे से घोंटने वाला) कहलाने लगा है; इस तरह उनका अंजाम इस बात की मिसाल बना कि सत्ता पर खुले व्यंग्य की उस दौर में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती थी। ज़टल्ली नरनौल (दिल्ली के क़रीब, आज का हरियाणा) के थे और वह औरंगज़ेब आलमगीर के अंतिम दौर से लेकर फ़र्रुख़सियर के ज़माने तक जीवित रहे।
कश्मीर के क्षेमेन्द्र की रचनाओं में भ्रष्टाचार, लूट, ढोंग और सामाजिक विघटन पर तीखा व्यंग्य है। क्षेमेन्द्र की आलोचना कश्मीर के राजा अनंतदेव (1028-1063 ई.) और कलश (1063-1089 ई.) के कालीन पतन पर केंद्रित थी। अनंतदेव के शासन में विद्रोह, आर्थिक पतन और नैतिक दिवालियापन चरम पर था, जिसे क्षेमेन्द्र ने, जिनके पूर्वज दरबारी थे, इन विसंगतियों को लोक-सुधार के मकसद से उभारा। क्षेमेन्द्र का व्यंग्य नैतिक पुनरुत्थान का आह्वान था।
इस संदर्भ में ‘मत्तविलास-प्रहसन’, ‘आगमडम्बर’, और क्षेमेन्द्र के प्रहसन कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि प्राचीन काल में भी धर्म के उपहास की एक परंपरा रही है, भले ही उस वक्त भी धर्म एक गंभीर मसला था। संस्कृत में स्वांग की विधा को प्रहसन कहते हैं जो विशेष रूप से धार्मिक विषयों से संबंध रखती है। ऐसी दो स्वांग रचनाएं ‘मत्तविलास-प्रहसन’ और ‘भगवदज्जुकम-प्रहसन’ का संबंध सातवीं शताब्दी के पल्लव शासक महेंद्रवर्मन से है। ‘मत्तविलास-प्रहसन’, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक मत्तविलासी कापालिक भिक्षु सत्यसोम के बारे में है जो कांची नगर में अपनी स्त्री-मित्र देवसोम के साथ घूम रहा है। स्त्री भी मत्त है। दृश्य में एक पागल के प्रवेश से अंत में बौद्धों, कापालिकों और पशुपतों का उपहास किया गया है। इन सभी को पतित, पाखंडी और बदमाश दिखाया गया है। यहां जॉनी वॉकर वाला सिनेमाई शराबी पात्र सत्यसोम के आदिम रूप में मौजूद है जो हाशिये के दार्शनिक की भूमिका में कुलीनों की पोल खोल रहा है।
ग्राम्यलोक का हास्य
सवाल है कि क्या गोनू झा, बीरबल, तेनालीराम आज भी गांवों में जिंदा हैं? और हैं तो क्यों? जवाब हो सकता है कि ये सिर्फ़ किस्से नहीं, बल्कि सामाजिक मॉडल हैं: बीरबल यानी सत्ता को बुद्धि से बेवकूफ़ बनाना, तेनालीराम यानी सत्ता के पाखंड को उजागर करना और गोनू झा यानी सत्ता के अहंकार पर वार करना। इन सब में एक बात समान है- अपनी बुद्धि से ताकतवर को हराना, जो प्रकारांतर से हास्यबोध भी पैदा करता है। गांव का आदमी खुद को इन्हीं में देखता रहा है।
शहरों में हास्य आज स्टेज, स्क्रीन और स्क्रिप्ट से आता है, जबकि गांव में हास्य जीवन से निकलता है। सबाल्टर्न सटायर है यानी ग्रामीण व्यंग्य जो मनोरंजन कम, ‘सर्वाइवल’ टूल अधिक है। गांव की औरतें खेत, चूल्हा, सास, पति, देवर, समाज सब झेलती हैं, इसलिए लोकगीतों में सास की तानाशाही, पति की निकम्मी मर्दानगी, समाज की दोगली नैतिकता, सबकी हँसी उड़ाई जाती है। किसान, मज़दूर, चरवाहा, ग्वाला, कुम्हार, धोबी- ये सब प्रकृतिक आपदाओं, कर्ज़, सामंती दबाव, जातिगत अपमान और अक्सर राज्य की उदासीनता के बीच जीते हैं। गांव का मजाक अक्सर सामाजिक हाइरार्की में ऊपर की ओर जाता है- जमींदार, ठाकुर, पटवारी, पुलिस, पंडित, नेता। कोई नहीं बचता, जैसे यह कहावत कि “पटवारी भगवान से ज्यादा जानता है।’’
अभाव के संदर्भ में सामंती सोच के दायरे में हास्यबोध की गंभीरता और बुद्धिचातुर्य की एक बानगी देखिए:
शादी के बाद पहली बार एक आदमी अपने ससुराल गया। साले-बहनोई घर में खाने बैठे। बर्तन जूठे होने के कारण साले की बहन ने एक ही थाली में खिचड़ी परोस दी और बीच में गड्ढा करके उसमें देशी घी डाल दिया। अब बहनोई सोचने लगा कि अगर किनारे से खाना शुरू करते हैं तो घी तो रह ही जाएग, और अगर बीच से खिचड़ी उठाते हैं तो साला उसे घी का लालची समझेगा (यहां घी को लग्जरी समझते हुए आगे बढ़ा जाए)। साला भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। अचानक बहनोई को एक आइडिया सूझा और उसने थाली में घी वाली जगह पर उंगली से तीन खड़ी रेखाएं खींचते हुए कहा– मैंने तीन चिट्ठियां भेजीं, लेकिन तुम्हारी तरफ से किसी का जवाब नहीं आया। साला भी मौके की तलाश में था। थाली में बेतरतीब उंगलियां घुमाते हुए झट बोल पड़ा– अरे, तुम इतना ‘गाजुर-माजुर’ (अस्त-व्यस्त, बेतरतीब) लिख कर भेजते थे कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो इस तरह उन दोनों ने प्रत्यक्ष तरीके से घी पर फोकस किए बिना पूरी खिचड़ी में घी को मिला दिया और खाना शुरू कर दिया।
गांव का हास्य कॉमेडी नहीं, एक गुप्त लोकतंत्र है, जहां जो खुलकर बोल नहीं सकता वह हँसकर सच कह देता है। हालांकि गांव अब पहले जितना खुलकर नहीं हँसता क्योंकि आज मजाक पर भी एफआइआर हो सकती है।
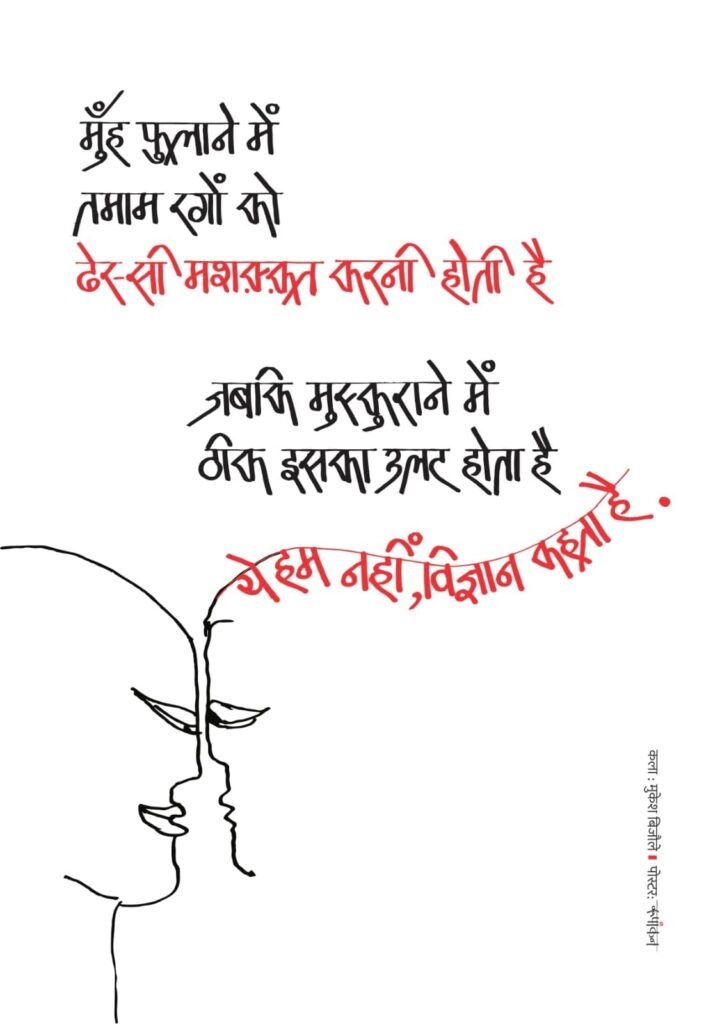
इतना कुछ होने के बावजूद, गार्डियन की रिपोर्ट और अचिन वनाइक की टिप्पणी एक हद तक सच क्यों लगती है? आखिर समाज में छाई मुर्दनी की वजह क्या है, चाहे जितनी भी हो? हमें भी कभी-कभार क्यों लगता है कि शुद्ध ठोस हास्यबोध गायब हो गया? क्या इसके लिए टीवी की स्क्रिप्टेड हँसी, व्हाट्सऐप के नफरती मजाक और वर्तमान राजनीति का डरावना दबदबा जिम्मेदार हैं?
समाजशास्त्रियों का कहना है कि भारत में एक गहरी ‘आज्ञाकारिता’ या फ़रमाँ-बरदारी की संस्कृति बढ़ी है- लोग शक्तिशाली व्यक्तियों या संस्थाओं को नाराज करने से डर रहे हैं। निजी जीवन में भारतीय भले ही हास्यप्रिय हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में यह डर हावी रहता है।







