आर्थिक तौर पर एक “नए भारत” की रचना करने वाले डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गोह नामक स्थान पर हुआ था (जो आज के पाकिस्तान में मौजूद है)। तक्सीम की सारी रूदाद अपनी आंखों से देखने और उस दर्द को महसूस करने की वजह से वह शांति की कीमत जानते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसी शांति को महफूज़ रखने के अथक प्रयास किए। वह भूख महसूस कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि करोड़ों भारतीय भूखे न सोयें। इन्हीं दो खूबियों ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में गढ़ा-बुना, पहले वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर। ये दो खूबियां ज़िंदगी भर उनके हर कार्य में झलकती रहीं।
पहले उनकी शिक्षा अमृतसर के हिंदू कॉलेज से हुई जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने शोध में इस बात की हिमायत की थी कि हिंदुस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा और खुला रखना चाहिए। आजकल के अकादमिक मनमोहन सिंह से कुछ सीख सकते हैं और अकादमिकों एवं आम लोगों के बीच के विभेद को मिटाने की ओर काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सुझाव अपनी थीसिस में सुझाए थे ताकत मिलने पर उन्होंने उन्हीं सुझावों को लागू करने पर पूरी शिद्दत के साथ काम किया।
अमेरिका में मनमोहन सिंह का एक शानदार करियर हो सकता था, मगर उसे छोड़कर उन्होंने हिंदुस्तान वापस आना चुना। 1970 की दहाई में वह दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में प्रोफ़ेसर की हैसियत से पढ़ा रहे थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया से उनकी पहली मुलाकात भी इन्हीं दिनों में हुई थी। उस वक्त इन दोनों के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि आगे चलकर इन दोनों की ऐतिहासिक साझेदारी भारत को एक गहरे आर्थिक संकट से उबारेगी। यूनाइटेड नेशंस में एक लुभावनी नौकरी छोड़कर भारत लौट कर पहले एक अकादमिक की हैसियत से और बाद में एक सरकारी मुलाज़िम की हैसियत से काम कर रहे मनमोहन सिंह उस वक्त तक अहलूवालिया के लिए एक आदर्श बन चुके थे। अहलूवालिया को सरकार के साथ उनकी पहली नौकरी के विषय में समझाने और बताने में भी मनमोहन सिंह ने अहम किरदार निभाया था।

जब इंदिरा गांधी ने 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तब मनमोहन सिंह को प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी सदस्य बनाया गया। इसके बाद 1982 में उन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस समय रुपये का विनिमय मूल्य एक बास्केट के संदर्भ में नापा जाता था जिस बास्केट में यूएस डॉलर, पाउंड-स्टर्लिंग, ड्यूटशे मार्क, येन तथा स्विस फ्रैंक हुआ करते थे। इस बास्केट की कीमत इस वक्त 100 रूपये की बराबर थी। मनमोहन सिंह ने पहली बार अहलूवालिया को इसी मुद्दे पर साथ लेकर ऐसा इंतज़ाम किया जिससे नॉमिनल एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलावों के लिए भी गुंजाइश रखी जा सके। इसे अहलूवालिया ने “क्रमिकवाद और गुपचुप सुधार” की संज्ञा दी है।
मनमोहन सिंह को जब राजीव गांधी के रूप में आधुनिकता की पैरवी करने वाला एक प्रधानमंत्री मिला तो उन्होंने यह राय रखी कि कृषि में आमूलचूल परिवर्तन और ग़ैर-कृषि सेक्टर में विकास किए बगैर आधुनिकता संभव नहीं है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता करने से पहले और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार बनने से पहले मनमोहन जिनेवा में साउथ कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे। जब पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। जब उन्होंने यह पद संभाला तब देश की अर्थव्यवस्था तितर-बितर हो रखी थी। भारत का बैलेंस ऑफ़ पेमेंट यानी दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान का हिसाब-किताब काफ़ी गड़बड़ हो चुका था और फॉरेक्स रिज़र्व बहुत तेज़ी से भूतल की ओर अग्रसर था। आइएमएफ़ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड) के साथ समझौता करना और उसकी शर्तों को मान लेना ही इकलौता रास्ता दिखाई पड़ता था। ऐसे में सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि रुपये का 9 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया। अवमूल्यन के एक और दौर के साथ ही कैश कंपनसेटरी सपोर्ट अर्थात निर्यात पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया गया।
एक नई इंडस्ट्रियल नीति लागू की गई और अर्थव्यवस्था को बाज़ार के लिए खोल दिया गया। अपनी बजट स्पीच के दौरान मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि फ़िसकल डेफ़िसिट को साल भर में 8.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत पर लाया जाएगा किंतु इसकी मार गरीबों पर नहीं पड़ेगी। इसके लिए कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत कर दिया गया और लग्ज़री आइटम जैसे एयर कंडीशनर और फ्रिज इत्यादि पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी गई। सेबी को एक वैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। मनमोहन सिंह का स्पष्टीकरण बहुत साफ़ था- पब्लिक सेक्टर विकास का इंजन होना चाहिए था मगर वह राष्ट्रीय संचय को लील जाने वाला गोदाम बन चुका था। अब समय आ चुका था कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं।
उदारीकरण की दलीलें
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से एक बहुत बड़ा बदलाव तो यह आया कि अब अधिक से अधिक विज्ञापन आने लगे जिसने टेलीविज़न का पूरा परिदृश्य ही क्रांतिकारी तरीके से बदल दिया और सरकारी चैनलों का एकाधिकार ख़त्म हुआ। इन बदलावों ने विकास को इस हद तक बढ़ावा दिया कि 2001 में जिम ओ’ नील की अगुआई में गोल्डमैन सैशे की रिसर्च टीम ने भारत को BRIC देशों (उस वक्त तक ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन) में से विकास के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाओं का देश करार दिया।
मनमोहन सिंह यह भली-भांति जानते थे कि उन्हें एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान लगा कर चले और इसीलिए उन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को आर्थिक मामलों का सेक्रेटरी बनवा दिया। जैसा कि अहलूवालिया ने अपनी किताब बैकस्टेज: दी स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ (2020) में बताया है, 1992- 93 में उठाए गए टैक्स संबंधी अहम कदम (राजा चेलिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर) निम्न थे-

1. निजी आय पर लगने वाले आयकर के स्लैब को चार से घटा कर तीन कर दिया गया।
2. वित्तीय संपत्ति पर लगने वाला वैल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया गया।
3. अधिकतम कस्टम ड्यूटी को डेढ़ सौ प्रतिशत से घटा कर 110 प्रतिशत कर दिया गया।
4. नए प्रोजेक्ट तथा आम यंत्रों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 80 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत कर दिया गया।
1995-96 तक भारत का औसतन आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) घट कर 36.6 प्रतिशत पर आ गया था लेकिन विकसित देशों के मुक़ाबले अब भी सुधार की गुंजाइश थी जहां यह औसत 15-18 प्रतिशत के बीच था। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि सर्विस सेक्टर का भी उदारीकरण हुआ था जिसकी वजह से इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस तथा एयर-ट्रैवल जैसे सेक्टरों में निवेश आना शुरू हुआ जिस पर पहले सरकार का ही एकाधिकार था। हालांकि बिना एक सेकेंडरी सेक्टर उत्पन्न किए इन सुधारों को लागू करने की कीमत भारत आज तक चुका रहा है, लेकिन इन सुधारों ने भारत को बहुत-कुछ नई दिशा में चलाने का काम किया है।
जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनी तो उसने आर्थिक सुधारों के प्रवर्तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। ऐसा होते ही मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री तथा इंदिरा गांधी और एच. डी. देवेगौड़ा के बाद राज्यसभा से चुने जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने सभी चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने के बजाय चली आ रही चीज़ों में ही थोड़े-बहुत संशोधन के साथ उन्हें अच्छा करने का प्रयास किया। लिहाज़ा हम उन्हें एफ़आरबीएम एक्ट, 2003 में कुछ बदलाव करके उसे और बेहतर बनाते हुए देखते हैं। यह बदलाव ऐसे थे- जैसे रिवेन्यू डेफ़िसिट को शून्य तक ले जाने का लक्ष्य और फ़िस्कल डेफ़िसिट को थोड़ा और घटाने का लक्ष्य आदि। खेल के ज़रिये डिप्लोमेसी अर्थात क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, उसे मनमोहन सिंह ने जारी रखा। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कश्मीर में पैदा हुए विश्वास पर और काम करते हुए वहां निजी सेक्टर के साथ मिलकर विकास की संभावनाओं पर काम करने की कोशिश की।
उनके दौर की सबसे अहम गतिविधियों में से एक थी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की शुरुआत। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में रोज़गार सुनिश्चित करना जिसके तहत हर वह ग्रामीण घर जिसके वयस्क सदस्य मजदूरी करने के लिए तैयार थे उन्हें 100 दिन का पक्का रोज़गार दिया जाना था। इसी के ज़रिये समुदाय की भावना को मज़बूत करके पंचायती राज व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की गई थी।
मनमोहन सिंह ने भारत की विस्तार पाती अर्थव्यवस्था में ऐसे इंतज़ाम किए थे कि वह बड़े से बड़े झटके झेल सकती थी। यही कारण है कि जब 2008 में दुनिया भर में आर्थिक तंगी आई और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर गई तब भी भारत की अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी हद तक बची रही।
विरोधाभास और सवाल
सवाल है कि क्या यह सब सुधार भारत के लिए अत्यंत लाभदायक ही साबित हुए? इसका बहुत निश्चित उत्तर देना न सिर्फ़ जल्दबाज़ी होगी बल्कि समकालीन भारत के साथ अन्याय भी होगा।
इसका कारण यह है कि मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने अर्थात बाज़ार की शक्तियों को अधिक और सरकार के दख़ल को कम जगह देने की पैरवी 1960 के दशक में की गई थी। अब सवाल उठता है कि कहा तो नेहरू के काल को ‘लाइसेंस राज’ जाता था (शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, 2016) किंतु जब हर तरफ़ सरकार का ही कब्ज़ा था तो भव्य निर्माण जो निजी निवेश द्वारा ही संभव था, कैसे हो पा रहा था?
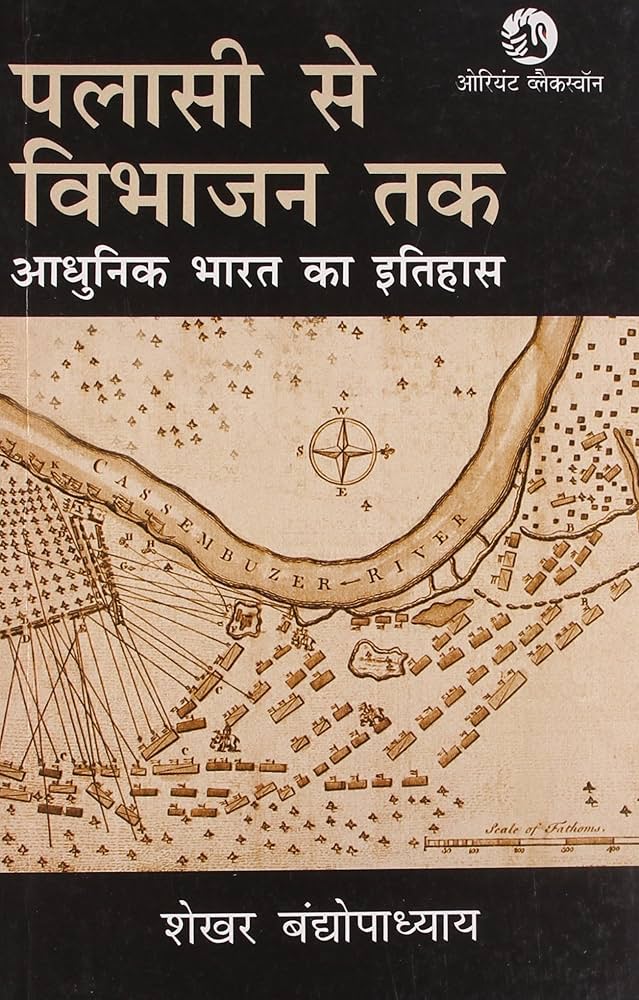
यहां यह बात बात याद रखना ज़रूरी है कि नेहरू के वक्त पहली पंचवर्षीय योजना आने पर संभावित विकास दर 2.2 प्रतिशत अनुमानित की गई थी लेकिन असल में विकास दर 4.9 प्रतिशत रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे नेहरू-महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है उसमें भी संभावित विकास दर अनुमानित से ज़्यादा ही रही। तब एक सवाल यह उठता है कि क्या मिक्सड इकॉनमी अर्थात एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों का समन्वय हो, भारत के लिए बेहतर नहीं थी?
इस बात से कुछ हद तक तो व्यक्ति सहमत हो सकता है, मगर 1991 के भारत की हालत को देखते हुए यह संभव नहीं था कि उदारीकरण से बचा जा सके। भारत 1991 की स्थिति में एक झटके में नहीं पहुंचा था, बल्कि दो बार 1980 के दशक में भी अर्थव्यवस्था को झटके लग चुके थे। इससे यह बात तो साफ़ हो जाती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार तो लाने ही थे, लेकिन उन्हें जिस तरह लागू किया गया वह परेशानी का सबब बन गया।
हरित क्रांति लाते वक्त यह बात साफ़ थी कि पूरे भारत भर के लिए ये सुधार नहीं लागू किए जा सकते थे। हरित क्रांति के लिए ज़रूरी चीज़ें थीं- बड़े खेत, मशीनों और उर्वरकों (फर्टिलाइज़र्स) का उपयोग और अधिक उत्पाद वाले बीजों (हाई यील्डिंग वैरायटी- HYV) का प्रयोग। अब यह सारी ही चीज़ें उन स्थानों पर मिल सकती थीं जहां लोगों के पास बड़ी ज़मीनें हों और खानदानी बड़े किसान ज़्यादा हों। लिहाज़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हरित क्रांति के गढ़ बने। आशा थी कि इन जगहों से आने वाली क्रांति के फ़ायदे धीरे-धीरे पूरे देश में बंट जाएंगे मगर अफ़सोस ऐसा हो न सका।
यही कारण है कि जब उदारीकरण पर ध्यान दिया गया तब यह उम्मीद जताई गई कि शायद कुछ बड़े सुधार कृषि में भी होंगे और यह उम्मीद तब और बढ़ी थी जब मनमोहन सिंह ने कृषि के बिना उदारीकरण को संभव करार दिया था। ताज्जुब ये कि उस वक्त से हरित क्रांति के कारण पनपी असमानताएं और ज़्यादा बढ़ने लगीं। एक नुकसान जो कृषि ने उठाया वो यह कि फ़सलें मौसम और स्थान के अनुरूप नहीं बल्कि बाज़ार की मांगों के अनुरूप होने लगीं। एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाती है। बिहार में गन्ने की उपज के लिए 27 राउंड पानी से ही काम चल जाता है परंतु तमिलनाडु में इसके लिए 40 राउंड पानी चाहिए होता है। लिहाज़ा न सिर्फ़ ये कि बाज़ार की ताक़तें फ़सलों के स्वाभाविक परिवेश से उन्हें दूर किए दे रहीं हैं वरन प्राकृतिक संसाधनों पर भी आघात कर रहीं हैं। यह एक बहुत बड़ी नकारात्मक देन है उदारवाद की।
एक और उदाहरण लेते हैं, जो आता है हरित क्रांति के नेपथ्य से जन्मी बीटी फ़सलों से, जो उच्चतम गुणों के बीजों के मेल से बनने वाले बीजों को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन बीजों पर बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, मगर जो चीज़ नहीं बताई जाती वो यह कि ये बहुत सारा पानी लील जाने वाली फ़सलें हैं। बाज़ार के कारण यह फ़सलें ऐसे स्थानों पर होने लगीं कि उस स्थान और वहां के किसानों के लिए काल साबित हुईं। बीटी कॉटन को मराठवाड़ा और विदर्भ में उगाने का काम किया जाने लगा (इसने 2001-2002 से ज़ोर पकड़ना शुरू किया) और साथ ही उठ खड़ी हुईं ऐसी दिक्कतें जिनसे आज तक यह क्षेत्र उबर नहीं सका है। बीटी फ़सलें लॉटरी के टिकट की तरह हो गईं। जिसकी लॉटरी लग गई उसके वारे-न्यारे जबकि जिसने टिकट अपने पास बचे पैसे से खरीदी थी उसके रंज और मलाल की सीमा नहीं।
साथ ही यह भी नहीं सोचा गया कि ऐसे क्षेत्रों में कम से कम लोन की व्यवस्था संगठित और सरकारी संस्थाओं से कराई जाए ताकि कुछ तो किसान को लाभ हो। यही कारण है कि ग़ैर-सरकारी और असंचालित संस्थानों से लोन लेने के कारण उस क्षेत्र के किसान आज तक आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। उन क्षेत्रों में बीटी फ़सलों को लाना ठीक ऐसे ही था कि बारिश के अभाव में फ़सलें न हों और गैलन भर पानी वानखेड़े स्टेडियम में मैच कराने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाज़ार के लिए जगह बनाते हुए भी यदि यह देखा जाता कि किस क्षेत्र में क्या स्थिति और कौन सी फ़सल सबसे बढ़िया होगी तो उत्पादन भी अच्छा होता, प्राकृतिक संसाधन भी बचते और मुनाफ़ा भी ठीकठाक होता- किसानों और उद्योग दोनों को ही।
समाजवादी सुधारों का वक्त
मौजूदा सरकार कृषि और इंडस्ट्री के बीच आधुनिक तकनीक लाकर कृषि की भलाई के लिए बहुत कुछ करने का दावा करती है पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एफ़पीओ यानी फ़ार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिन पर मौजूदा सरकार ने और अधिक काम किया है, उनकी परिकल्पना और स्थापना दोनों ही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी।
अब इसमें दिक्कत ये है कि उद्योगपति कभी-कभी किसानों को चकमा देते हैं और किसान उन्हें शंका से ही देखते हैं। उदारवाद से शुरू हुए इन तमाम बाज़ारवादी ताक़तों के कृषि में दख़ल का चरम हाल में आए तीन कृषि कानूनों की शक्ल में परिणत हुआ। चूंकि उसमें किसान के हित कम थे और शंका बहुत अधिक इसीलिए सरकार को इन तीन क़ानूनों को वापस लेना पड़ा। लिहाज़ा कृषि पर उदारीकरण का मूलतः सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि किसान को कहीं कोई मुनाफ़ा नहीं हुआ, मगर एक समग्र विकास जो न सिर्फ़ आमदनी बल्कि खुशहाली, पर्यावरण का संरक्षण, सभी क्षेत्रों का उनकी भौगौलिक स्थिति के अनुसार विकास इत्यादि को भी बढ़ावा देता, वह नहीं हो सका।
सेकेंडरी सेक्टर, जो किसी भी मुल्क में आर्थिक विकास की आधारशिला होता है, उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आप इसे यूं समझिए कि एक शानदार बहुमंज़िला इमारत तामीर करने का ख़्वाब आप देखते हैं। अब ज़ाहिर है उसकी तामीर के लिए आधारशिला मज़बूत होनी चाहिए और उसके ऊपरी तल ठोस और विशाल होने चाहिए। मगर इन दोनों मज़बूत और भव्य निर्माणों को जोड़े रखने के लिए जिन खंभों की आवश्यकता पड़ेगी यदि वो जर्जर हों या फ़र्ज़ कीजिए हों ही न, तब इमारत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था वही इमारत है जिसमें खंभा रूपी सेकेंडरी सेक्टर पहले तो गायब ही था और अब जर्जर अवस्था में है। इसीलिए कृषि आज भी हमारी राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान देती है और उससे भी बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो सर्विस सेक्टर (सेवाओं) का है, जबकि एक विकसित देश की पहचान होती है कि कृषि, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इसी क्रम में बढ़ोत्तरी का योगदान दें।
जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत में उदारवाद से होने वाले नुकसान उससे उपजे फायदों पर भारी पड़ते रहेंगे क्योंकि विकास के साथ-साथ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की असमानता और बढ़ती चली जाएगी। मध्यम वर्ग में एक जैसे ठीकठाक हालात वाला वर्ग घने से घना होने चाहिए तभी उदारवाद का कुछ फ़ायदा है और ऐसा कुछ अन्य देशों में देखा भी गया है। भारत में भी यही प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी भारत का समग्र विकास और उदारवाद का कोई फ़ायदा हो सकेगा। इसीलिए अब एक और आर्थिक सुधार के दौर का वक्त आ चुका है। इस दौर में मात्र उदारवाद से काम नहीं चलेगा, समाजवाद के कुछ अंग विशेष जैसे सरकार का सकारात्मक हस्तक्षेप आदि साथ में ले कर चलना अत्यंत आवश्यक है।


