कृषि उपज बाजार समिति (APMC) कानून सहित तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर साल भर तक चले दुनिया के सबसे बड़े किसान आंदोलन के झटके चुनावी मौसम में अब बिहार तक पहुंच गए हैं। बिहार में मौजूदा विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच ‘इंडिया’ गठबंधन और महागठबंधन के घटक राजनीतिक दलों ने अपने 32 पन्ने के संयुक्त घोषणापत्र में “APMC अधिनियम की बहाली” और कृषि बाजार समितियों को फिर से सक्रिय करने का वादा किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद यह वादा बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 को निरस्त करने की एक तार्किक और आश्वस्तकारी ज़मीन तैयार करता है।
संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिहार में 2006 में कृषि उपज मंडी (निरसन) अधिनियम लागू किया गया था। विश्व बैंक समूह के प्रभाव में राज्य की सभी विपणन समितियों और विपणन बोर्डों को बिना किसी अध्ययन के अचानक भंग और नष्ट कर दिया गया था। एपीएमसी कानून निरस्त होने के बाद राज्य में कृषि उपज के विपणन के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रह गई और न ही कोई शुल्क लिया जा सकता है। सरकारी विनियमन के अभाव में कृषि बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
पुराने नियामक विपणन ढांचे को पुनर्जीवित करने की अनिवार्यता विशेष रूप से कर्नाटक कृषि उपज विपणन (विनियमन और विकास) (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 6 मार्च, 2024 को राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद उभरी है, जिसे 7 मार्च, 2024 को कर्नाटक गजेट एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी में प्रकाशित किया गया था। इससे पता चलता है कि कर्नाटक सरकार ने तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन का अनुकूल जवाब दिया। कर्नाटक का यह कानून मूल बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 को वापस लेने और फिर से लागू करने की एक नजीर पेश करता है।
इसे जरूर पढ़ें
कृषि मंडियों पर कर्नाटक का फैसला और विपक्षी एकता के संयोजक के लिए एक सबक
एपीएमसी के ‘बाईपास’ कानून
बिहार एपीएमसी कानून के निरस्तीकरण ने रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, विधायिका और न्यायपालिका की सिफारिशों पर ही सवाल उठा दिया, जिन्होंने कृषि बाजारों के विनियमन की सिफारिश की थी और जिसके आधार पर देश भर में एपीएमसी कानूनों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। बिहार एपीएमसी निरसन विधेयक का विपक्षी दलों ने राज्य विधानसभा में प्रदर्शन कर के बाकायदे विरोध किया था। इस कानून के विरोध में पटना की सड़कों पर एक लंबा विरोध जुलूस भी निकाला गया था, उसके बावजूद विधेयक पारित कर दिया गया! निरसन अधिनियम 1 सितंबर, 2006 को बिहार गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्रकाशित किया गया और वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020- सवालिया तीन केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक- दरअसल एपीएमसी कानून के एक बाईपास जैसा था, ठीक वैसे ही जैसा एपीएमसी निरसन कानून है। 2020 का यह ‘बाईपास’ एपीएमसी कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही रोक लगा दी है, एपीएमसी मार्केट यार्ड/सब-यार्ड के बाहर एक नया “व्यापार क्षेत्र” बनाता था जहां पैन संख्याधारी कोई भी खरीदार सीधे किसानों से उपज खरीद सकता था। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को इस तरह की लेनदेन पर कोई टैक्स लगाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था।
इस केंद्रीय बाईपास एपीएमसी कानून के समर्थकों ने दावा किया था कि यह कानून खरीदारों के लिए खरीद लागत को कम करेगा जिसका मतलब अपने आप किसानों के लिए उच्च कीमतें होंगी। तथ्य यह है कि कम लागत पर खरीदारी करने वाले खरीदारों का मतलब यह नहीं है कि वे खरीद पर बचाई गई लागत किसानों को दे देंगे। यह दावा कि इससे किसानों को एक विकल्प मिलेगा, भ्रामक था क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को छोड़कर पूरे भारत में अधिकांश कृषि उत्पादक एपीएमसी के माध्यम से नहीं जाते हैं। पैनधारी किसी भी व्यक्ति को कृषि उपज खरीदने की अनुमति दी गई थी, जिससे उपज की जमाखोरी का मार्ग प्रशस्त हो गया था। जमाखोरी का हानिकारक प्रभाव तो कई पुरानी भारतीय फिल्मों का विषय रहा ही है।
इतना ही नहीं, जब किसी व्यापारी या कमीशन एजेंट को लाइसेंस दिया जाता है तो एक काउंटर पार्टी जोखिम आश्वासन होता है। एपीएमसी कानून के तहत अगर किसानों के भुगतान को लेकर कोई विवाद होता है तो एपीएमसी इसका संज्ञान लेती और उसे हल करने का प्रयास करती थी। यहां तक कि मॉडल राज्य कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2003 भी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से विपणन समिति को यह सुनिश्चित करने के अधिकार देता है कि व्यापारी अपनी क्षमता से अधिक कृषि उपज न खरीदें, उपज के निपटान में विक्रेताओं को जोखिम से बचाएं, तथा खरीदारों की क्षमता के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में आवश्यक नकद सुरक्षा प्राप्त करने के बाद ही लाइसेंस प्रदान करें।
बाईपास कानून ने ऐसी मूल्यवान संस्थागत परंपराओं को नजरअंदाज किया। अंतत:, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केंद्रीय बाईपास एपीएमसी कानून पर रोक लगाई और बाद में उसे निरस्त कर दिा, तब जाकर बिहार एपीएमसी निरसन कानून के खिलाफ उच्च अदालतों में दाखिल अपीलों की तार्किक वैधता पुष्ट हो सकी। गौरतलब है कि केंद्रीय बाईपास एपीएमसी कानून 2020 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में से एक था जिसे किसानों के अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण प्रधानमंत्री को एक वर्ष के भीतर ही माफी मांगनी पड़ी और अधिनियम को वापस लेना पड़ा था।
बिहार में एपीएमसी को कैसे खत्म किया गया
1960 का बिहार एपीएमसी कानून कृषि और संबद्ध वस्तुओं में निष्पक्ष व्यापारिक लेनदेन सुनिश्चित करने हेतु बाजारों के निर्माण के लिए बनाया गया था। कानून का मुख्य उद्देश्य ऐसी विपणन समितियों को नियुक्त करना था जो विनियमित बाजारों के कामकाज की निगरानी के लिए उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय अधिकारियों और सरकार की प्रतिनिधि हों। इसके उद्देश्य में बाजार शुल्कों का विनियमन और अतिरिक्त शुल्कों की वसूली पर रोक लगाना, बाजार प्रथाओं का विनियमन, बाजार अधिकरणों को लाइसेंस देना और खुली नीलामी द्वारा बिक्री के अलावा बाजार यार्ड में विश्वसनीय और अद्यतन बाजार जानकारी के प्रदर्शन की व्यवस्था शामिल थी।
मॉडल अधिनियम के अनुरूप अपने एपीएमसी कानून में संशोधन करने के बजाय बिहार, 2006 में एपीएमसी कानून को समाप्त करने वाला एकमात्र राज्य बन गया। यह केवल निजी कंपनियों को एक संकेत भेजने के लिए किया गया था क्योंकि विश्व बैंक के एक अध्ययन ने स्वीकार किया था कि “एपीएमसी अधिनियम को बिहार में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए बड़ी बाधा नहीं माना जाता है (अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत)’’। इस अध्ययन में कहा गया था कि “बाजार सुधार उपज की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि, निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ बेहतर बाजार प्रबंधन, उच्च बाजार निवेश गतिविधि और संभवतः अधिक विकसित आपूर्ति श्रृंखलाओं में उच्च रोजगार सृजन को सक्षम करेगा। उसने यह भी दावा किया था कि बिहार एपीएमसी कानून को निरस्त करने से सेवा प्रदाताओं के लिए मूल्य श्रृंखलाओं के हित अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैकवर्ड लिंकेज और प्रोत्साहन के विकास की सुविधा होगी, जिसके चलते किसानों को प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरित किया जा सकेगा।
इसके बाद बिहार कृषि उत्पाद मंडी (निरसन) विधेयक, 2006 10 अगस्त, 2006 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। विपक्षी दलों के रामदेव वर्मा, जगदानंद सिंह और महेश्वर सिंह जैसे विधायकों ने राज्य विधानसभा में निरसन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया और विधेयक को काला कानून करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने रामदेव साय, लालबाबू राय और रामदास राय जैसे विधायकों के विधेयक को एक महीने के भीतर जांच के लिए विधायी समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। इसके बाद विपक्ष के सभी विधायकों ने विधेयक के विरोध में नारेबाजी करते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। इस कानून के विरोध में पटना की सड़कों पर एक लंबा विरोध जुलूस भी निकाला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण के बाद विधायिका ने विधेयक पारित कर दिया।
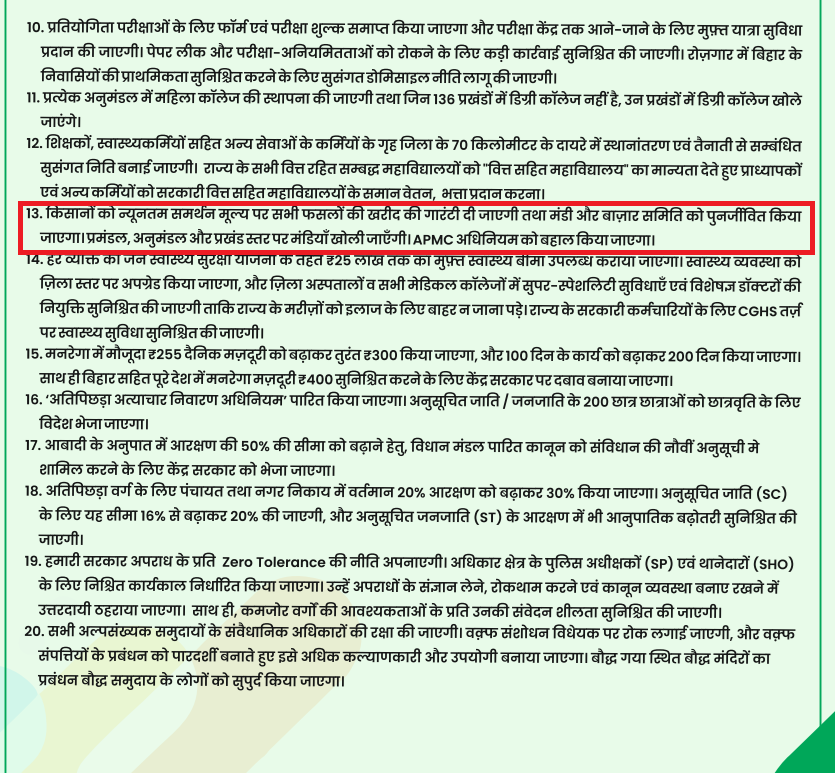
तब अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कृषि विकास और कृषि विपणन के विकास के लिए मौजूदा कानून को निरस्त करना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया था कि जिस उद्देश्य से एपीएमसी अधिनियम बनाया गया था और किसानों की जमीन ली गई थी, वह पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो दल राज्य में विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार के अंग के रूप में इसका समर्थन कर रहे हैं जो इस काम को करना चाहती है। उन्होंने इस संबंध में बैंकरों की एक राज्यस्तरीय बैठक में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ हुई चर्चा का जिक्र भी किया। उन्होंने वादा किया कि एपीएमसी अधिनियम के तहत अधिग्रहित और बनाई गई संपत्ति का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
इस निरसन अधिनियम द्वारा, बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960, और उसके तहत बनाए गए 1975 के नियमों को निरस्त कर दिया गया था, सिवाय पटना उच्च न्यायालय के 2017 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 12655 के कुछ फैसलों को छोड़कर। निरसन अधिनियम की वैधता को चुनौती तो दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इसे एक अच्छा कानून माना गया था और इसे अधिकारातीत करार दिया गया।
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार कंठ ने तर्क दिया था कि निरसन अधिनियम को लागू करने के कारण के बतौर यह कहा गया है कि 1960 का अधिनियम कृषि उपज मंडियों के विनियमन के अपने उद्देश्यों में विफल रहा है जबकि यह कारण किसी भी मौजूदा साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि निरस्त होने के समय विपणन बोर्ड ने 197 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा कर ली थी जिससे पता चलता है कि बिहार कृषि उपज बाजार बोर्ड अच्छी तरह से काम कर रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि निरसन अधिनियम का उद्देश्य बाजार बोर्ड की संपत्ति का अधिग्रहण करना है। उन्होंने बताया कि 2006 के निरसन अधिनियम को लागू करने से पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि 1960 के बिहार एपीएमसी अधिनियम में 1982 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली गई थी इसलिए अधिनियम को निरस्त करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता है। चूंकि “राष्ट्रपति की आवश्यक पूर्व मंजूरी” नहीं ली गई, इससे स्पष्ट है कि बिहार एपीएमसी निरसन अधिनियम के मामले में एक वैध कानून को लागू करने में संवैधानिक जनादेश का पालन नहीं किया गया है।
एपीएमसी के बाद का दौर
2006 में बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 को निरस्त करने के साथ, ‘’यह उम्मीद की जा रही थी कि इससे निजी कंपनियां बाजार स्थापित करने और चलाने में सक्षम होंगी। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हुआ।‘’ राज्य में एपीएमसी मंडी प्रणाली के समाप्त होने के बाद राज्य के किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
बिहार एपीएमसी अधिनियम के उन्मूलन से पहले बिहार में 95 मार्केट यार्ड थे जिनमें से 54 में कवर्ड यार्ड, गोदाम और प्रशासनिक भवन, तौल, प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाइयां जैसे बुनियादी ढांचे हुआ करते थे। 2004-2005 में राज्य कृषि बोर्ड ने करों के माध्यम से 60 करोड़ रुपये कमाए और 52 करोड़ रुपये खर्च किए। खर्च किए गए धन में से 31 प्रतिशत बुनियादी ढांचे के विकास पर था। एपीएमसी कानून को निरस्त करने के बाद एपीएमसी बेमानी हो गया और बुनियादी ढांचे की कमी ने किसानों की आय को कम कर दिया। कुल 129 पूर्ववर्ती बाजार समितियां अस्तित्वहीन हो गईं, जिससे किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
इसे भी पढ़ें
बिहार सरकार झूठ बोल रही है या घर लौट कर खाली बैठे लाखों प्रवासी मजदूर?
2006 में एपीएमसी कानून को समाप्त करने से कृषि उपज की खरीद पर सरकार की निगरानी खत्म हो गई। उससे पहले कृषि उपज बाजार समिति द्वारा नियंत्रित मंडियों (थोक बाजारों) के माध्यम से महत्वपूर्ण मात्रा में खरीद की जाती थी, जहां किसान सीधे अपनी उपज को भारतीय खाद्य निगम या राज्य कृषि निगम को स्थापित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेच सकते थे। यह उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाता था। एपीएमसी अधिनियम के उन्मूलन के बाद 8,463 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) और कुछ पंचायत स्तर की समितियां बनाई गईं जो कृषि उपज की खरीद में मध्यस्थ का कार्य करती हैं; वे किसानों से उपज खरीद कर एफसीआइ, एसएफसी और निजी संस्थाओं को बेचती हैं। कहां इसका उद्देश्य किसानों की रक्षा करना और उनकी आय को बढ़ाना था, पर वास्तव में किसानों को निजी खिलाड़ियों के आने, सरकारी एजेंसियों द्वारा बिलों के असामयिक भुगतान और औने-पौने दामों पर संकटग्रस्त बिक्री के चलते उलटे और कम कीमत मिलने लगी।
एपीएमसी उन्मूलन से पहले के दौर में किसान स्थानीय मंडियों में जगह के लिए मामूली शुल्क पर आवेदन करते थे, जिसे निर्वाचित और सरकार द्वारा नामित सदस्यों वाली एक बाजार समिति द्वारा चलाया जाता था। यह बाजार समिति बिहार कृषि विपणन बोर्ड की देखरेख और नियंत्रण में थी जिसने एमएसपी को सख्ती से लागू करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, एपीएमसी के पास कृषि उपज के भंडारण के लिए जगह थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि किसान अपनी उपज को लाभकारी मूल्य पर बेचने में देरी कर सकते थे और उसी दिन उनका भुगतान किया जाता था जिस दिन वे अपनी उपज बेचते थे।
पैक्स प्रणाली में तो शुरुआत से ही पंजीकरण के साथ जटिलताएं और अनियमितताएं बड़े पैमाने पर चालू हो जाती हैं। इसके लिए उस भूमि के दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिस पर किसान खेती करते हैं। यह डिजिटल पैक्स खरीद प्रणाली से कई किसानों को बाहर छोड़ है, उन इलाकों में जहां इंटरनेट का घनत्व कम है। यह “इंटरनेट की पर्याप्त पहुंच और प्रभावी उपयोग” के आधार पर किसानों के बीच लाभान्वितों और वंचितों का नया वर्ग गढ़ता है।
बिहार में एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करने से पहले और बाद में मूल्य रुझानों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि धान, गेहूं और मक्का की कीमत और एमएसपी के बीच का अंतर या तो बढ़ गया है या 2006 के पूर्व-एपीएमसी स्तर पर ही बना हुआ है। 2007-08 और 2016-17 के बीच दस विपणन सीजन में, बिहार में एक भी सीजन में कीमत एमएसपी से अधिक नहीं देखी गईं। चार सीजन में कीमत एमएसपी का 90 प्रतिशत या उससे अधिक रही। दूसरी ओर पंजाब में, इस अवधि के दौरान दो सीजन ऐसे रहे जब कीमत एमएसपी से अधिक हो गईं, जबकि केवल एक सीजन में कीमत में एमएसपी के 90 प्रतिशत से नीचे की गिरावट देखी गई। 2007-08 और 2016-17 के बीच दस सीजन में, एपीएमसी अधिनियम के उन्मूलन के बाद बिहार में कीमत तीन सीजन में एमएसपी के 70-80 प्रतिशत के भीतर थीं, और शेष छह सीजन में एमएसपी के 80-90 प्रतिशत के बीच थीं।

यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि बिहार में राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि उपज के लिए खरीद केंद्रों की संख्या 2016 में 9,000 से घटकर 2020 में 1,619 हो गई। ऐसे में एमएसपी की अनिश्चितता और मुक्त बाजार के प्रति अविश्वास को लेकर किसानों की बढ़ती चिंता समझ में आती है। किसानों को कृषि उपज का कम मूल्य मिलने के परिणामस्वरूप बिहार में कृषि मजदूरी कम हो गई। जबकि 2006-07 में बिहार में एक खेतिहर मजदूर की औसत मजदूरी पंजाब में मजदूरी का लगभग 79 प्रतिशत थी, वर्तमान में बिहार में एक खेतिहर मजदूर को पंजाब में एक खेतिहर मजदूर को मिलने वाली मजदूरी का 61 प्रतिशत मिलता है।
बिहार के बदहाल किसान
एपीएमसी कानून को निरस्त करने के खिलाफ किसानों के विरोध की आवाज बिहार में मुखर इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सूबे में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग किसी तरह जीवन निर्वाह करता है।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) की बिहार इकाई के सितंबर 2021 के एक परचे में बताया गया है कि बिहार में 90 प्रतिशत किसानों के पास 1 हेक्टेयर (2.47 एकड़/3.95 बीघा) से कम भूमि है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए भूमि और पशुधन जोत सर्वेक्षण (2012-13) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण बिहार में औसत जोत का आकार सिर्फ 0.242 हेक्टेयर है, जो 2012-13 में 29 राज्यों के बीच चौथा सबसे छोटा था। नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 (एनएएफआइएस) के अनुसार, बिहार में प्रति परिवार औसत भूमि 0.5 हेक्टेयर है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मूल्य केवल 35,825 रुपये है, जबकि अकेले पंजाब में यह 78,652 रुपये है। स्पष्ट रूप से, पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मूल्य बिहार की तुलना में दोगुने से अधिक था। नाबार्ड के सर्वे से पता चलता है कि बिहार में एक किसान की औसत मासिक आय 7,175 रुपये थी, जो पंजाब में 23,133 रुपये है।
MSP: आंदोलन से भी नहीं खिला सूरजमुखी, मक्का-मूंग पर बढ़ रहा है गुस्सा
राज्यों के कृषि विपणन मंत्रियों की समिति की आठवीं बैठक (30 अक्टूबर, 2012 को आयोजित) में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआइएएम), जयपुर के निदेशक एम.एस. जयरथ ने एपीएमसी अधिनियम से वंचित राज्यों में बाजार सुधारों और बाजार विकास की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने “बिहार में एक नियामक तंत्र की आवश्यकता’’ पर जोर दिया जिसकी ‘’प्रकृति अपेक्षाकृत विकासात्मक होनी चाहिए’’। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान व्यवस्था किसानों के हित में नहीं है और इसके लिए व्यवस्थित विपणन की आवश्यकता है। उक्त बैठक में कृषि विभाग सचिव, बिहार ने कहा कि “कोई नियामक प्रणाली नहीं होने के बावजूद किसानों को अब भी लाभकारी मूल्य मिल रहा है।‘’ हालांकि, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार श्रबनी गुहा को लिखे एक बाद के पत्र (दिनांक 22 मई, 2020) में बिहार के कृषि विभाग के सचिव एन. सरवण कुमार ने यह उल्लेख किया कि नियामक प्रणाली के अभाव में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।
राज्य मंत्रियों की समिति की नौवीं और अंतिम बैठक (22 जनवरी, 2013 को आयोजित) में एनआइएएम ने पाया कि बिहार जैसे राज्यों में कृषि बाजारों में अपेक्षित विपणन अवसंरचना, संगठित सूचना प्रसार, सामान्य रखरखाव और सुव्यवस्था का पूर्ण अभाव है। चूंकि बाजार अनियंत्रित होते हैं, इसलिए किसानों पर उनकी उपज के लेन-देन में उच्च कमीशन शुल्क लगाया जाता है। इन बाजारों के किसी भी पेशेवर प्रबंधन के अभाव में किसानों को उच्च लेनदेन शुल्क, मूल्य और आवक आदि पर जानकारी के अभाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। एनआइएएम ने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में बाजारों को पूर्ण नियंत्रणमुक्त करने से लेनदेन की लागत कम करने के बजाय वास्तव में इसमें वृद्धि हुई है। इससे इन बाजारों में निजी क्षेत्र से किसी भी निवेश को आकर्षित करने में मदद नहीं मिली है। यह कहते हुए एनआइएएम ने एक कानूनी और संस्थागत संरचना की आवश्यकता पर बल दिया जो राज्य में कृषि बाजारों का विनियमन कर सके और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को भी आकर्षित कर सके।
11 सितंबर, 2021 को पटना में बिहार राज्य सम्मेलन में प्रस्तुत एआइकेएससीसी के परचे में दावा किया गया कि 2006-21 के दौरान बिहार के किसानों को सात लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। परचे में कहा गया है कि बिहार में 35 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम भूमि है। चूंकि वे केवल अपने जीविका के लिए उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी कृषि उपज को लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर नहीं मिलता है। यद्यपि वे लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए किसानों के संघर्ष का समर्थन करते हैं, वे जानते हैं कि एमएसपी की घोषणा केवल 23 फसलों के लिए की गई है लेकिन सरकारी खरीद कुल मिलाकर गेहूं और धान तक सीमित है। बिहार में किसान लंबे समय से लाभकारी मूल्य से वंचित हैं। एपीएमसी से पहले और बाद की अवधि में, किसानों को अपनी उपज स्थानीय आढ़तियों और कमीशन एजेंटों को बेचने के लिए बाध्य किया गया है।
बिहार के किसान विपणन योग्य इतने अतिरिक्त माल का उत्पादन करते हैं जिसे एपीएमसी मार्केट यार्ड में लाया जा सकता है, लेकिन उन्हें परिवहन सुविधा की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई होती, तो अधिशेष उत्पादन करने वाले किसान एपीएमसी मार्केट यार्ड के लाभार्थी बन सकते थे। सरकार को किसानों को आश्वासन देना चाहिए था कि उनकी उपज खरीदी जाएगी। बिचौलिये को हटाने और खरीद के आश्वासन के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करने के बजाय एपीएमसी अधिनियम को ही बदल दिया गया। किसानों ने बेशक विरोध किया और उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में कानून के निरसन को चुनौती दी, पर बिहार में बड़ी संख्या में किसानों के बीच संसाधनों और जागरूकता की कमी हाल के दिनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों जैसे विरोध का रूप नहीं ले सकी।
कृषि बाजारों की जमीन पर कब्जा
कृषि उपज के भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के बजाय बिहार कृषि बाजार यार्ड भूमि हस्तांतरण अध्यादेश, 2017 ला दिया गया जिसके माध्यम से दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र और उद्यान के निर्माण की परियोजना शुरू की गई।
इसके अंतर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार की कृषि बाजार यार्ड भूमि, जो बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 द्वारा राज्य सरकार की है, उसे स्थायी रूप से पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। अध्यादेश की अनुसूची से पता चलता है कि पटना शहर में मार्केट यार्ड के लिए अधिग्रहित 10 एकड़ भूमि को 20 सितंबर, 2017 को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, दिसंबर 2017 में बिहार कृषि बाजार यार्ड भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 2017 लागू किया गया था।
डीसी, हजारीबाग उर्फ अदाणी के मुलाजिम बनाम अन्य
बिहार कृषि बाजार यार्ड भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 2017 की आवश्यकता बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 की धारा 4(vi) के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें कहा गया है कि “बोर्ड या समिति की सभी अचल संपत्तियों का उपयोग केवल कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना सहित किसान से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिनमें बागवानी, कृषि सेवा, कृषि विपणन, कृषि उपज का भंडारण शामिल हैं।‘’ धारा 4(i) के अनुसार, उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख से और उसके द्वारा चल और अचल स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियां, जिनके बोर्ड या समिति से संबंधित होने का दावा किया गया है, वे राज्य सरकार में निहित होंगी। सांविधिक और गैर-सांविधिक, सुरक्षित या असुरक्षित सहित सभी देयताएं राज्य सरकार की देयता होंगी।
बिहार कृषि बाजार यार्ड भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 2017 ने गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि बाजार यार्ड भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दी, जिससे 2,400 एकड़ से अधिक शेष कृषि बाजार यार्ड भूमि (ऊपर बताए गए 10 एकड़ आवंटित करने के बाद) और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। एपीएमसी कानून को निरस्त करने के बाद, ‘प्रशासक’ या विशेष अधिकारी को एपीएमसी कानून के तहत समितियों की ऐसी सभी संपत्तियों की कस्टडी दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा बाजार समितियों का प्रभार कृषि उपज मंडियों के क्षेत्र में संबंधित उप-मंडल अधिकारियों को सौंपा गया था। यह स्पष्ट है कि बिहार कृषि उपज (निरसन) अधिनियम, 2006 का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि बाजार यार्ड भूमि के हस्तांतरण के लिए किया जा रहा है। यह कानून की मूल मंशा के विपरीत है। यह कृषि भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के प्रति स्पष्ट असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।
यह आशंका है कि 2,400 एकड़ शेष कृषि बाजार यार्ड भूमि अदाणी समूह जैसी संस्थाओं को दे दी जाएगी। बिहार सरकार ने 2,400 मेगावाट की कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना के लिए अदाणी पावर लिमिटेड को भागलपुर जिले के पीरपैंती में 1,050 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का फैसला किया है। यह जमीन, केवल एक रुपये प्रति एकड़ के वार्षिक किराये पर 33 साल के लिए पट्टे पर दी गई है। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि इससे सरकार को सालाना 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। राजस्व के नुकसान के अलावा, इससे क्षेत्र में गंभीर जल संकट पैदा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 2010-212 के दौरान पांच पंचायतों से भूमि का अधिग्रहण किया था। इसी अवधि के दौरान बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया था। ‘इंडिया’ और महागठबंधन का घोषणापत्र बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव से बेखबर है, जिसे 2012, 2020 और 2025 में संशोधित किया गया है।
एपीएमसी निरसन से पहले के दौर में, 95 विनियमित एपीएमसी बाजारों में से 54 बाजारों में बुनियादी विपणन बुनियादी ढांचा था। ये 54 बाजार करीब 1595 एकड़ जमीन में स्थापित किए गए थे। करीब 813 एकड़ जमीन खाली थी। अब जब गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि बाजार यार्ड भूमि का हस्तांतरण शुरू हो गया है, तो यह बहुत संभव है कि एपीएमसी कानून के निरसन से पहले मौजूद बुनियादी ढांचे का भी गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। एपीएमसी के बाद की अवधि में मार्केट यार्ड की भूमि भी अतिक्रमण का सामना कर रही है।
बिहार के कृषि विभाग और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के बीच पत्राचार उपरोक्त चिंताओं की पुष्टि करता है। मई 2020 में उनके बीच हुए पत्राचार से पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए बिहार एपीएमसी कानून को निरस्त किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ है। यह देखा गया है कि एपीएमसी कानून को निरस्त करने से विशेष रूप से धान की कीमतों में कमी आई है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जब एपीएमसी कानून अस्तित्व में था, तब भी विनियमित बाजारों में बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता थी। हालांकि, इनके सुधार के लिए सार्वजनिक निवेश किया जा रहा था। एपीएमसी कानून को निरस्त करने से पहले, चूंकि उच्च परिवहन लागत किसानों को मंडियों में जाने से हतोत्साहित करती थी, इसलिए किसानों के आसपास पीएमसी यार्ड और सब-यार्ड स्थापित करने और/या उन्हें मुफ्त परिवहन प्रदान करने के प्रयास किए गए थे। एपीएमसी कानून के निरस्त होने से पुरानी मंडियों को समाप्त करके एपीएमसी अधिनियम के प्रवेश के अवरोध को हटा दिया गया। उम्मीद थी कि इस निरसन से कृषि विपणन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निजी निवेश होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी उम्मीदें गलत हैं।
बेगूसराय और खगड़िया से एक समाचार रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि किसान छोटे व्यापारियों को अनाज बेचते हैं, जो इसे बोरे में भरकर बड़े कमीशन एजेंटों-सह-व्यापारियों को आपूर्ति करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 2 नवंबर, 2020 को रिपोर्ट की, “एपीएमसी निरसन का दूसरा पक्ष: बिहार के किसान ‘पंजाब की तरह’ मंडियां चाहते हैं’’ ताकि प्रोसेसर/मिल मालिक केवल बड़े व्यापारियों के साथ सौदा करें। वे सीधे किसानों से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, हालांकि बिहार के कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम ने इसकी अनुमति दी है। एपीएमसी निरस्त कानून के बाद निजी व्यापारियों द्वारा संचालित बिहार की एकमात्र सक्रिय मंडी – जिसमें सार्वजनिक संस्थानों की कोई निगरानी नहीं है – पूर्णिया के पास गुलाब बाग में है। 2005-06 के आसपास यह मध्य अप्रैल से मध्य जुलाई तक मक्का के पीक सीजन के दौरान रोजाना 3-4 रेल रेक को संभालती थी। 2,600 टन के इन रेक को पूर्णिया, रानीपत्र और जलालगढ़ रेलवे स्टेशनों से लोड किया जाता था। वर्तमान में लोडिंग केवल एक रेक तक जा चुकी है। वहां बेचने वालों में से लगभग 80 प्रतिशत किसान 20-25 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और शेष 20 प्रतिशत स्थानीय व्यापारी हैं। जाहिर है कि पटना सिटी मार्केट यार्ड की तरह गुलाब बाग भी आने वाले समय में इतिहास बनने के लिए तैयार है। बिचौलियों, कमीशन एजेंटों को खत्म करने के बजाय एपीएमसी के बाद की अवधि बड़े और अनियंत्रित कृषिव्यवसायियों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गई है, जो नए बिचौलियों के रूप में उभरे हैं।
कृषि-क्षेत्र में सरकारी भूमिका का एहसास
यह याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के कारण ही जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास एपीएमसी कानून सहित केंद्रीय कृषि कानूनों को निलंबित कर दिया था। ऐसे में यह समझ आता है कि अगर बिहार एपीएमसी कानून को निरस्त करने की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया होता, तो उसका भी यही हश्र होता। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बलिया और न्यायमूर्ति बारिन घोष की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, खासकर इस आधार पर कि निरसन कानून की संवैधानिकता पर किसानों की प्रार्थना के विशिष्ट पहलुओं पर अभी तक फैसला नहीं किया गया है।
बाईपास एपीएमसी कानून को निलंबित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2021 के आदेश, बिहार एपीएमसी कानून को असंवैधानिक रूप से निरस्त करने की पुष्टि करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश और बिहार के कृषि विभाग व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच हुए पत्राचार का संयुक्त अध्ययन बिहार में एपीएमसी कानून को वापस लाने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करता है, जिसकी मांग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) की बिहार इकाई ने 26 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति को भेजे अपने ज्ञापन में की थी। इसके पक्ष में एनसीएईआर का अध्ययन भी सरकार द्वारा हस्तक्षेप का तर्क मुहैया करवाता है, जो कहता है कि “बाजार को स्थिर करने के लिए खरीद शुरू की जानी चाहिए। सरकार द्वारा इस तरह के संचालन के लिए ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ स्थापित करना उपयोगी होगा।‘’ वास्तव में, यह बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम को असंशोधित रूप में वापस लाने के लिए एक मजबूत तर्क देता है।
एपीएमसी कानून को निरस्त करने के बाद पिछले 15 वर्षों का अनुभव इंगित करता है कि विश्व बैंक के निदान और नुस्खे अपर्याप्त थे। इन अपर्याप्तताओं का जवाब देते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट सभी 54 बाजार प्रांगणों (विपणन यार्ड) के विकास के लिए कार्यक्रमों का प्रस्ताव करके कृषि विपणन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को संबोधित करता है। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित 2,446 करोड़ रुपये का उपयोग करके निष्पादित करने का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (COMFED) और कुछ निजी उद्यमों की मदद से सामान्य सुविधा केंद्र बनाने में निवेश कर रही है। यह भंडारण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। बिहार राज्य बीज निगम भी एक सुविधा केंद्र का निर्माण कर रहा है। राज्य सरकार मानती है कि कृषि विपणन और किसानों के कल्याण के लिए भंडारण सुविधाएं और गोदाम महत्वपूर्ण हैं। बिहार राज्य भंडारण निगम राज्य की भंडारण एजेंसी है। 2020-21 के दौरान सरकारी स्वामित्व वाले गोदामों की उपयोग क्षमता 77.8 प्रतिशत थी।
यह भी पढ़ें
‘वोट चोरी’ और SIR के आर-पार, क्या सोच रहा है चुनावी बिहार? जमीनी स्वर और शुरुआती संकेत…
कुल मिलाकर, सरकारें अब यह पहचानने लगी हैं कि एपीएमसी दरअसल कृषि क्षेत्र में सरकार की बुनियादी भूमिका से ताल्लुक रखता है। एपीएमसी का कृषि से वही रिश्ता है, जैसा शिक्षा के साथ सरकारी स्कूल का है। कृषि क्षेत्र में एपीएमसी स्वास्थ्य क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की तरह है। विशेष रूप से महामारी के सबक और सामान्य रूप से लगभग समूची आबादी की स्वास्थ्य देखभाल इस बात को रेखांकित करती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का कोई विकल्प नहीं है। उसी तरह, सरकारी स्कूल दोषपूर्ण हैं, उनमें कई कमियां हैं, उनके पास शौचालय नहीं हैं, 80 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए उचित शौचालय नहीं हैं, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है- इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी स्कूलों को खत्म ही कर दिया जाए और उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। यह तथ्य शिक्षा पर कम बजटीय आवंटन के लिए कोई तर्क नहीं बनाता ताकि निजी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यह एक तथ्य है कि सरकारी स्कूल खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी खराब हैं। वे लाखों बच्चों के लिए एकमात्र आशा हैं। वे मिड-डे मील की एकमात्र आशा हैं- दिन में केवल एक अच्छा भोजन।
सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का सबक राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि बाजारों पर भी लागू होता है क्योंकि एक नियामक के रूप में अकेले सरकार की उपस्थिति ही किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी सुनिश्चित कर सकती है। जिस तरह स्कूलों और अस्पतालों को परिष्कार और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होती है, एपीएमसी को भी परिशोधन और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के साथ एपीएमसी की तुलना आर्थिक न्याय, समता और समानता का एक अहम पाठ है।
किसान बनाम करोड़पति-अरबपति

बिहार में विपक्षी दलों के घोषणापत्र में किए गए एपीएमसी संबंधी वादे इस रोशनी में भी महत्वपूर्ण हो उठते हैं कि मार्च 2025 में प्रकाशित द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपये है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक-तिहाई है और बिहार की जीडीपी का लगभग दस गुना है।
बिहार में अरबपतियों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (एसआइएस) लिमिटेड के संस्थापक आरके सिन्हा और अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के संस्थापक महेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसके अलावा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 – चरण I के विश्लेषण से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन दाखिल करने वाले 1303 उम्मीदवारों में से 519 (40%) करोड़पति हैं।
प्रमुख दलों में जन सुराज पार्टी के 114 उम्मीदवारों में से 81 (71 फीसदी), राजद के 70 उम्मीदवारों में से 68 (97 फीसदी), जदयू के 57 उम्मीदवारों में से 52 (91 फीसदी), भाजपा के 48 उम्मीदवारों में से 44 (92 फीसदी), बसपा के 89 उम्मीदवारों में से 27 (30 फीसदी), कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों में से 18 (78 फीसदी), आम आदमी पार्टी (आप) के 44 उम्मीदवारों में से 13 (30 फीसदी), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 13 उम्मीदवारों में से 10 (77 फीसदी), सीपीआइ के 5 उम्मीदवारों में से 3 (60 फीसदी), सीपीआइ (एम) के 3 उम्मीदवारों में से 2 (67 फीसदी) और सीपीआइ (एमएल-लिबरेशन) के 14 उम्मीदवारों में से 2 (14 फीसदी) ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है।
इसीलिए मार्च 2023 में लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज द्वारा प्रकाशित लीड जर्नल में प्रकाशित ‘’जर्नी ऑफ एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी लॉ इन बिहार” और जुलाई 2023 में पटना से प्रकाशित सबाल्टर्न जर्नल में प्रकाशित “बिहार में कृषि मंडियों के खात्मे की एक पड़ताल” शीर्षक वाले शोधपत्रों ने मूल बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम को फिर से लाए जाने के लिए एक मजबूत पक्ष रखा था, ताकि भारत के 284 अरबपतियों की बढ़ती हुई कमाई के बीच किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय में आ रही अभूतपूर्व गिरावट के सामने किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। उपर्युक्त तथ्य, एपीएमसी कानून के तहत सार्वजनिक संस्थानों की ऑडिट रिपोर्ट और तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के निरस्तीकरण ने बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 को मूल रूप में पुनर्जीवित करने का फिलहाल एक मंच तैयार कर दिया है।







