जब यह आलेख लिखा जा रहा है, तो छठे चरण का मतदान हो चुका है और केवल एक चरण का मतदान बाकी है। यानी, मतदाताओं ने नयी सरकार का फैसला ईवीएम की पेटियों के सुपुर्द कर दिया है। अब, बस नतीजों का आना बाकी है, हालांकि इस दौरान एक ऐसा बयान, एक ऐसी परिघटना भी हुई जिसे किसी ने नहीं छुआ, लेकिन वह किसी बम-धमाके से कम नहीं था।
पांचवे चरण के मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा ने यह दावा कर दिया कि भाजपा अब अपने बूते काम करने में समर्थ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर उसकी निर्भरता नहीं रही है। इस बयान के निहितार्थ बड़े गहरे हैं, लेकिन कमाल की बात यह रही कि भारत के विपक्ष से लेकर तथाकथित मीडिया ने भी इस बयान को ऐसे पचा लिया मानो जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान से प्रेरित होकर ही ‘आत्मनिर्भर भाजपा’ का मंत्र फूंक दिया है।
जगतप्रकाश नड्डा के इसी बयान से अगर पहले चरण के मतदान के ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को मिलाएं तो तस्वीर के कई कोण उभरते हैं। सरसंघचालक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा क्योंकि कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का संघ का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इससे भी आगे जाकर यह ऐलान कर दिया कि संघ को कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में 100 वर्ष लगे, जो कि बेहद चिंताजनक है। वैसे, सांत्वना देने के लिए उन्होंने इस मंद गति का ठीकरा 2000 वर्षों के सामाजिक पतन पर ही फोड़ा।
संबंधित कहानी
निन्यानबे का फेर : फीकी रामनवमी, कम मतदान और भागवत बयान की चुनावी गुत्थी
सरसंघचालक के इस बयान और नड्डा के ‘आत्मनिर्भर भाजपा’ के बीच की कड़ी अगर आप खोजना चाहें, तो मार्च 2024 में हुई संघ की प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक को याद करना चाहिए जहां शताब्दी वर्ष को पुरजोर और असरदार तरीके से देशव्यापी बनाने के तमाम तरीकों पर चर्चा हुई, कार्यक्रम तय किए गए। उसके बाद भागवत के बयान से लेकर नड्डा के बयान तक गंगा-जमुना में टनों सीवर बह चुका है, चुनाव के छठे चरण तक बात मंगलसूत्र से मुजरे और संविधान बचाने से आरक्षण का दायरा धार्मिक आधार पर करने तक की बात हो चुकी है, लेकिन इस एक परिघटना को अगर देखें तो उसके मायने और संदर्भ बहुत गहरे हैं।
आगे बढ़ने से पहले यह बात हमें समझनी होगी कि भाजपा और संघ का नाभिनाल संबंध नहीं है। बात अगर केवल सांगठनिक स्तर पर जन्म की हो, तो संघ का जहां शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है, वहीं भाजपा के अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। भाजपा के पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ की भी बात करें तो वह भी संघ से बहुत बाद में पैदा हुआ। संघ हमेशा खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है (और हाल-फिलहाल तक रहा भी है) और यही वजह है कि जो लोग स्वाधीनता-संग्राम में संघ की ‘राजनीतिक संबद्धता’ पर सवाल पूछ कर उसे अक्सर कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं वे नादान हैं।
संघ का ध्येय वाक्य एक शब्द में अगर सूत्रबद्ध करें तो वह हिंदू स्वयंसेवकों की ऐसी फौज तैयार करना था जो समाज में व्यापक और स्थायी परिवर्तन ला सके ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने के उसके प्रकल्प पर काम किया जा सके (एक बार फिर से कहना होगा कि यह हाल-फिलहाल तक वैसा ही था, लेकिन समय की गति से यह लक्ष्य भी बदला है और अब तो संघ का एक अंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है)।
संघ-भाजपा: इतिहास, अंतर्संबंध और राजनीति
संघ की स्थापना के पीछे मोपला के दंगे थे। उसी के बाद एक हिंदू संगठन बनाने की बात हुई, जो हिंदू हितों पर काम करे और मुसलमानों और ईसाइयों को ‘काउंटर’ कर सके।
ध्यान रहे कि आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार खुद कभी कांग्रेस और हिंदू महासभा में भी रहे थे। उनके वैचारिक गुरु बालकृष्ण शिवराम मुंजे इटली के फासिज्म से प्रभावित थे। वह चाहते थे कि देश की युवा पीढ़ी सैन्य अभियान को समझे, उसमें भाग ले और सैन्य स्तर पर तैयार रहे। फासीवाद से प्रभावित होने की बात को नकार भी दें, तो हेडगेवार मुंजे से तो प्रभावित थे ही। अगर फासीवादी दस्तों को जाने दें, तो स्काउट्स के प्रारूप को ही संघ ने अपनाया। ड्रेस से लेकर ड्रिल तक, संघ पर उसकी छाप देख सकते हैं।
हेडगेवार की वीर सावरकर से बहुत अधिक वार्ता हुई और उन्होंने तब ही कांग्रेस की तरह एक राजनीतिक दल बनाने की सलाह दी। यह आजादी के पहले की बात है। जब हेडगेवार नहीं माने तो सावरकर नाराज भी हुए। तभी उन्होंने अपना बहुचर्चित वाक्य भी कहा था कि एक स्वयंसेवक पैदा स्वयंसेवक होता है, रहता स्वयंसेवक है और मर भी स्वयंसेवक ही जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल ही किसी सैन्य संगठन की तर्ज पर बना था। यह बहुत ही गुप्त प्रकार का संगठन होता था (शायद अब भी है)। इसमें एक सरसेनापति होता था जो सलामी लेता था। यह समय के साथ कमोबेश घटा, पर इसके ढांचे में वह सैन्य आत्मा आज भी मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि संघ और उसके राजनीतिक संगठन या स्वयं संघ के भीतर ही विवाद नहीं हुए। जब हेडगेवार रामकृष्ण मिशन के एक संन्यासी गुरु गोलवलकर को सरसंघचालक बनाकर लाए, तो स्वयं संघ के अंदर ही संघर्ष हुआ। गुरु गोलवलकर परकाया-प्रवेश हैं, संघ की प्रक्रिया से नहीं आए हैं- ऐसी बातें भी कही गयीं, हालांकि तब (यानी आजादी तक) राजनीति बहुत ही ध्रुवीकृत थी। मुसलमानों का प्रश्न उस समय की राजनीतिक में केंद्रीय था, हालांकि उस समय भी ‘डिस्कोर्स’ को संघ लीड नहीं कर रहा था, हिंदू और हिंदुत्व के विचार को उस समय आर्य समाज नेतृत्व दे रहा था, द्वितीयक तौर पर हिंदू महासभा थी- जो राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय थी और काम कर रही थी- और इन दोनों के बाद तीसरे स्थान पर संघ था।
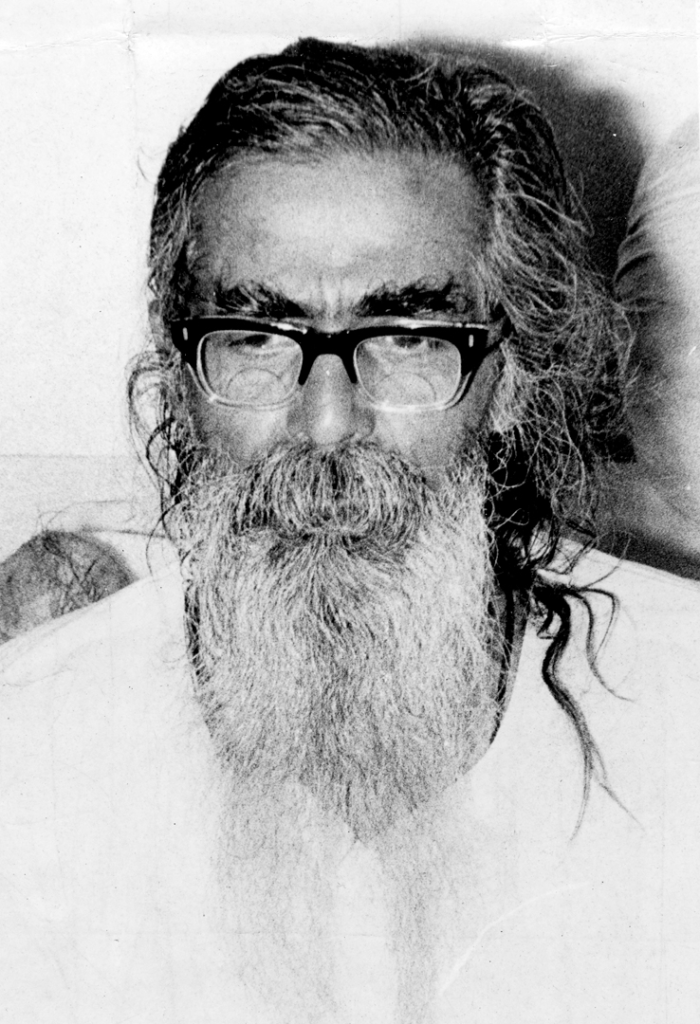
गोलवलकर ने ध्रुवीकरण पर काफी काम किया। उन्होंने वैचारिक और सामाजिक स्तर पर संघ को गुहांधकार से निकाला और उसकी प्रस्थापनाएं बनायीं वरना अब तक तो संघ एक व्यक्ति के दिमाग का फितूर ही था। इसलिए उसी समय की राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा।
हिंदू महासभा की तरफ से श्यामाप्रसाद मुखर्जी आजादी के बाद गांधी के कहने पर नेहरू कैबिनेट में गए, हालांकि तब उनको महसूस हुआ कि एक स्वस्थ लोकशाही के लिए सबल विपक्ष जरूरी है और उन्होंने अपनी अलग पार्टी ‘जनसंघ’ बनायी। जब वह पार्टी बना रहे थे, तब समान विचारों वाले सभी संगठनों से संपर्क किया और उसी क्रम में संघ से भी संपर्क किया। तब तक एक संगठन के रूप में संघ की ख्याति ऐसी हो चुकी थी कि माना जाता था इसमें समर्पित और आस्थावान कार्यकर्ता होते हैं। मुखर्जी ने तब कुछ कार्यकर्ता संघ से मांगे और तब संघ ने दीनदयाल उपाध्याय, भाई महावीर जैसे लोगों को दिया और भारतीय जनसंघ में ये लोग गए।
संघ की एक और विशेषता थी, प्रचारकों की। वे प्रचारक ही काम करने जाते थे। इन प्रचारकों के माध्यम से जनसंघ पर आरएसएस ने नियंत्रण किया। संघ को फायदा यह हुआ कि राजनीतिक पार्टी के लॉञ्च होने के साथ ही सामान्य जनता तक संघ पहुंचने लगा और धीरे-धीरे वह सब से बड़े हो गए। यह स्वाधीनता के पहले दो दशकों में हुआ। सांस्कृतिक संगठन को राजनीति का समर्थन मिला और वह विशाल होता चला गया। फिर, संगठन मंत्री भेजे जाने लगे और वे नियंत्रण करने लगे। इस समय जो हायरार्की यानी पदानुक्रम था, उसमें पहले स्थान पर संघ था, दूसरे पर जनसंघ और तीसरे पर ही बाकी संगठन या व्यक्ति आते थे।
दीनदयाल, वाजपेयी और संघ
अटलजी की राजनीति शुरू हुई श्यामाप्रसाद मुखर्जी का पीएस बनने से, लेकिन उनका वक्तृत्व और करिश्मा धीरे-धीरे संघ की सरहदों को पार करता चला गया। पूर्व सरसंघचालक रज्जू भैया ने तो अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि संघ के प्रचारक, कार्यकर्ता अटलजी के भाषण सुनने जाते थे और उनकी कविताओं का प्रचार करते थे।
जनसंघ में दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका भी बहुत बड़ी है। सभ्यतागत विचार और विचारधारा के स्तर पर समझ बहुत व्यापक थी। उनके और गोलवलकर के विचार मिलते थे, बल्कि कई बार तो भ्रम सा प्रतीत होता है कि किसने आखिर किसको प्रभावित किया। दीनदयाल की लोकप्रियता अधिक थी और गठबंधन सरकारों पर काम शुरू हुआ। 1967 में जनसंघ राष्ट्रीय फलक पर एक वैकल्पिक संगठन के तौर पर उभरा। उसी वर्ष पहली बार कांग्रेस के आधिपत्य को चुनौती मिली थी और जनसंघ ने तीन दर्जन से अधिक सांसद जिताये थे, हालांकि तभी दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी और जनसंघ का विजय-रथ जो पूरी रफ्तार से चल रहा था उसकी गति में रुकावट आ गयी।
उनकी मौत के पीछे कई तरह की ‘कांस्पिरेसी-थियरीज’ आयीं और जनसंघ के दिग्गज नेता बलराज मधोक (जो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जनसंघ का दीया जलाते रहे) ने तो सीधा-सीधा आंतरिक राजनीति की ओर इशारा कर दिया था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि चूंकि ‘दीनदयाल रूपी नथ संघ रूपी नाक से भारी हो गयी थी’ इसलिए संघ इस मामले में क्लीन चिट नहीं पा सकता है।
बहरहाल, दीनदयाल के बाद तीन सत्ता-केंद्र बने। पहला संघ, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरा लालकृष्ण आडवाणी। जहां कहीं भी द्वंद्व की स्थिति आती थी, आडवाणी-अटल मिल जाते थे और संघ को दबा देते थे। अभी तक जनसंघ से लेकर भाजपा तक संघ की ठसक इतनी जरूर थी, इतना असर जरूर था कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बाद से तब तक कार्यकर्ताओं को वैधानिकता (लेजिटिमेसी) और स्वीकार्यता संघ ही देता था। यानी, संघ की प्रक्रिया से निकलना अनिवार्य था, तभी आप जनसंघ यानी भाजपा में ऊंचे कद और पद पर जा सकते थे।
1980 में अटल-आडवाणी का कद इतना बढ़ा कि राज्यों में भी उनकी चलने लगी, लेकिन निचली इकाइयों पर संघ का नियंत्रण कायम रहा। संगठन मंत्री पर अब भी संघ का ही बोलबाला था। कद और वरिष्ठता का भी मसला होता था। बालासाहब देवरस ने एक बार मिसेज कौल वाले मसले को भी लेकर मीटिंग बुलाई थी, जिस पर अटलजी ने बाकायदा व्यक्तिगत मामले का हवाला देकर पूरे रूखेपन से उस पर किसी भी तरह की चर्चा होने से मना कर दिया। जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, तो पहले स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। नंबर दो पर फिर भी संघ था और उसके बाद तीसरे स्थान पर लालकृष्ण आडवाणी थे।
नब्बे का दशक और राम मंदिर आंदोलन
राममंदिर आंदोलन के बाद जब अशोक सिंहल राजनीतिक पटल पर आए, ‘विवादित ढांचे’ का विध्वंस हुआ और भाजपा एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ताकतवर हुई, तो संघ फिर से पहले स्थान पर आ गया। रथयात्रा के बाद आडवाणी नंबर वन बने और संघ रक्षात्मक हो गया। अटलजी वैसे भी संगठन से अधिक चुनावी-राजनीति के व्यक्ति थे और संघ के ही एक विचारक के शब्दों में- ‘मुखौटा’ थे।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही सुदर्शन (सरसंघचालक) और अटल-आडवाणी में संघर्ष होने लगा। संघ चूंकि ‘विवादित ढांचे’ के विध्वंस के बाद अपनी सफाई दुनिया को देना चाहता था या कहें अपने बारे में बताना चाहता था, तो उसी समयावधि में पहली बार संघ ने अपना प्रवक्ता (प्रचार-प्रमुख) मा.गो. वैद्य को बनाया, हालांकि वैद्य और वाजपेयी की सरकार में काफी ठनी रही और कई बार तो सुदर्शन भी अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर देते थे। अटलजी की भ्रू बंकिम होने का ही परिणाम था कि आखिरकार 2003 में वैद्य को हटाकर संघ को राम माधव की भर्ती करनी पड़ी (राम माधव के बाद प्रवक्ता किस्म का पद भी संघ में खत्म ही हो चला है)।
इस युग में संघ की दखल खत्म हो गयी, हालांकि जिला स्तर पर उनका नियंत्रण रहा। 2004-2014 की अवधि में अटल चूंकि बीमार पड़ गए थे, आडवाणी जिन्ना की मजार पर मत्था टेक कर ‘बे-साख यानी डिस्क्रेडिट’ हो चुके थे, तो संघ का नियंत्रण अंतिम और सर्वोच्च हो गया। मोदी युग के आने और डिस्कोर्स को तय करने के पीछे का इतिहास भी देखना होगा।
संबंधित कहानी
1992 के बाद बौद्धिक हस्तक्षेप के संकट पर आनंदस्वरूप वर्मा से बातचीत
अयोध्या के युद्ध में: साधु और शैतान के बीच फंसा भगवान
2002 में गोधरा के बाद जब मोदी को अंग्रेजी मीडिया (कथित लुटियंस मीडिया या खान मार्केट गैंग) द्वारा ‘शैतान’ बनाया गया और देशी मीडिया (खासकर हिंदी और गुजराती) ने उनको नायक बनाया, तो भारतीय राजनीति में एक नयी परिघटना हुई। मोदी की छवि उनके व्यक्तित्व से भी बड़ी हो गयी और वह इतनी बड़ी ‘इमेज’ बनी कि पहली बार हिंदुओं को यह लगा कि वे मुस्लिमों और ईसाइयों को ‘काउंटर’ कर सकते हैं। यही तो संघ का मूल विश्वास, मूल मुद्दा और मूल लक्ष्य था- हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों और मार्क्सवादियों को ‘हिसाब’ से रखा जा सके।
इस विचार के सबसे बड़े बल्कि एकमात्र प्रतिनिधि नरेंद्रभाई दामोदरदास मोदी बने। इसके बाद 2014 और 2019 की जीत ने उनको ‘लार्जर दैन लाइफ’ बनाया और अब उनकी टक्कर खुद उन्हीं से हो रही है। वह ‘भूतो न भविष्यति’ हो गए और ऐसा अटल-आडवाणी युग में भी नहीं हुआ था, न ही श्यामाप्रसाद-दीनदयाल युग में। इसीलिए, संघ और मोदी का टकराव तो अनिवार्य था।
मोदी-काल: संघ का समर्पण
आज जो नड्डा का बयान आया है, वह जाहिर तौर पर उनकी ‘हैसियत’ नहीं है। इसके पीछे मोदी की ताकत है। मोदी और संघ का झगड़ा तो गुजरात में ही शुरू हुआ था और इसकी बड़ी वजह यह है कि संघ की सबसे ब़ड़ी खूबी या खामी जो भी कहिए, वह ‘नियंत्रण’ की है। ‘कंट्रोल’ के बिना संघ को और किसी भी चीज से मतलब नहीं है और संघर्ष यहीं से शुरू हुआ।
मोदी की मर्जी नहीं थी, तो मनमोहन वैद्य को संघ को वापस लेना पड़ा। संजय जोशी को भी संघ ‘टैसिटली’ सपोर्ट करता था क्योंकि ‘कंट्रोल’ उसके लिए सबसे जरूरी है। वह मानता है कि नागपुर में जुकाम हुआ तो दिल्ली में लोग परेशान हों। अक्सर लोग कहते हैं न कि आप लड़ते-लड़ते खुद दुश्मन की तरह बरताव करने लगते हैं। संघ जीवन भर वामपंथियों से लड़ा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मॉस्को में बारिश होने पर छाता खोल लेते थे। संघ की चाहत भी वही है, कि नागपुर में बारिश हो तो दिल्ली में छाता खुले।

उसी तरह, दूसरे स्तर पर देखिए तो अगर कोई गुलाम है, तो काम तो कर रहा है, लेकिन गुस्सा तो होता ही है। नरेंद्र मोदी भी गुलाम भले थे, लेकिन स्वाधीनता की चाहत तो रही ही होगी। संघ के साथ सबसे बड़ी समस्या रही है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही के बिना वह सत्ता का सुख भोगना चाहता हैं। मोदी के बाद यह समस्या ही खत्म हो गयी कि संगठन और मातृ-संगठन पर कौन हावी होगा। 2014 के बाद मोदी ही यत्र-तत्र-सर्वत्र थे। वही मुद्दा थे, वही मसला भी और वही मुंसिफ भी।
अपार लोकप्रियता ने उनको वह ताकत भी दे दी कि वह सीधे तौर पर जो कहते थे, वही होता था। सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण किसी भी दौर ने नहीं देखा था। यहां तक कि अमित शाह भी जब अध्यक्ष बने तो उनको अरुण जेटली और संघ के जरिये लॉबींग कर के सत्ता पर कब्जा बनाना पड़ा। अमित शाह मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन मोदी वह नहीं चाहते थे। आखिरकार, अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बन सके।
संघ की सत्ता-लिप्सा और भविष्य
2014 के बाद संघ की पहुंच भी अकूत और अकथ तरीके से बढ़ी। शाखाओं से लेकर ऊपर तक संघ दोगुनी गति से बढ़ा। राजनीति में एक कहावत है कि शब्दों से अधिक उन शब्दों के इशारों को समझना चाहिए। नड्डा का यह संदेश सीधा संघ को है कि लकड़ी करना बंद करो। इसकी वजह यह है कि संघ का नियंत्रण अब बूथ लेवल तक भी नहीं रहा। जो संघ पहले भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी तक की नियुक्ति कर सकता था, वह अब बूथ अध्यक्ष तक नहीं बना सकता है।
इसके अतिरिक्त इस भ्रम का भी टूटना जरूरी है कि संघ ही भाजपा की रीढ़ है। आप इतिहास देख लीजिए, संघ हमेशा शहरी मध्यमवर्ग तक ही सीमित रहा है। आज भी आप गांवों में जाकर संघ के बारे में पूछिए तो शायद ही आपको कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन भाजपा और मोदी के बारे में अब भारत के कोने-कोने में बताने वाले लोग मिल जाएंगे। इसीलिए, यह जो धमकी दी जाती है कि संघ अगर बैठ गया तो भाजपा बैठ जाएगी, खोखली है। संघ की मानें, तो इस बार भी वह बैठा ही हुआ है, लेकिन चुनाव नतीजों में वैसा नहीं दिखेगा।
इसे भी पढ़ें
बिहार : संघ-भाजपा की दाल यहां अकेले क्यों नहीं गल पाती है?
संघ का एकमात्र योगदान था कि वह समर्पित कार्यकर्ता मुहैया कराता था। बूथ तक के स्तर पर वह कार्यकर्ता मुहैया कराता था, झंडे-बैनर लगाता था, दरी बिछाता था, जुलूस में जाता था और वोटर को निकाल कर बूथ पर लाना, वगैरह करता था। अब तो भाजपा वह कर ले रही है, बल्कि बूथ अध्यक्ष बनने के लिए भी लंबी कतारें लगी हैं। अब तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को ही समाहित करे, यही मसला नहीं सुलझ पा रहा है। फिर, भाजपा भला संघ के लोगों को कहां से समाहित करेगी, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों करेगी?
इसीलिए संगठन मंत्रियों ने भी अपनी निष्ठा बदल ली है। राजनीति में सबसे अधिक निष्ठा मायने रखती है। चीजें उसी दिशा में चल रही हैं। संघ के लोगों को सत्ता की आदत पड़ गयी है। इसमें अगर गतिरोध पैदा किया जाएगा तो 90 फीसदी कार्यकर्ता असहयोग करने लगेंगे और संघ की दीवारें दरक उठेंगी। नड्डा का बयान चूंकि संघ को करीब से जानने औऱ देखने वाले ही ‘डीकोड’ कर पाएंगे, इसलिए ही इस बयान पर कोई हंगामा नहीं बरपा है क्योंकि इसको लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
पुनश्च
इन पंक्तियों के लेखक की जब इसी मसले पर एक वामपंथी चिंतक और पत्रकार से बात हो रही थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि राहुल गांधी इसको मुद्दा इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि क्या पता संघ अब उन पर ही दांव लगा दे- आखिर संघ एक सांस्कृतिक संगठन ही तो है, जो राष्ट्र-निर्माण के लिए किसी भी राजनीतिक शाखा पर दांव लगा सकता है।
उन्होंने भले मजाक में यह बात कही, लेकिन यह बहुत दूर की कौड़ी भी नहीं है। आखिर संघ ही वह संगठन है जिसके कार्यकर्ताओं अशोक मिश्र और सभापति विश्वकर्मा ने तब लालू प्रसाद यादव के प्रस्तावक के तौर पर सेवा दी थी, जब वह छपरा से पहली बार चुनाव लड़े थे। लालू यादव के अलावा 1974 के आंदोलन के किसी भी छात्र नेता को टिकट नहीं मिला था, लेकिन लालू अपवाद बने, उसके पीछे भी संघ का ही आशीर्वाद था। यहां तक कि संघ के स्वयंसेवक सोहम प्रेस में एकत्रित होते थे और लालू के चुनाव अभियान का वहीं से संचालन होता था। स्वयंसेवकों ने ही चंदा कर के लालू के कपड़े भी बनवाए थे। 1990 में भाजपा के 39 विधायकों का समर्थन भी लालू को मिला था, तब वे मुख्यमंत्री बने थे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की किताब में तो यह भी दावा किया गया है कि 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को भी संघ ने समर्थन दिया था।
अब अगर संघ किसी नये घोड़े पर दांव लगाना चाहे, तो इसे बिल्कुल गप नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बहुत मेहनत और साधना का काम है जो दस साल से सत्ता सुख भोग रहे संघियों से संभव नहीं दीखता।
[लेखकीय स्पष्टीकरणः इस आलेख के लिए कई लोगों से बातचीत की गयी, जिसमें संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान सरकार में वरिष्ठ पदों पर मौजूद नौकरशाह और राजनेता शामिल हैं। जिन्हें दक्षिणपंथी खेमे का पत्रकार माना जाता है, उनसे भी बात हुई है। कुछ ऐसे राजनीतिक अध्येताओं से बात हुई जो संघ के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। पता नहीं क्यों आजकल उनको संघ-विचारक कहने का फैशन चल पड़ा है। इस लेखक के हिसाब से संघ विचारक नामक कोई चीज नहीं होती है। बहरहाल, इनमें से किसी ने भी अपना नाम छापने पर सहमति नहीं जतायी, इसलिए उक्त लेख में किसी का नाम नहीं दिया गया है। उनके दिए बयान कहानी का अंग हैं।]







